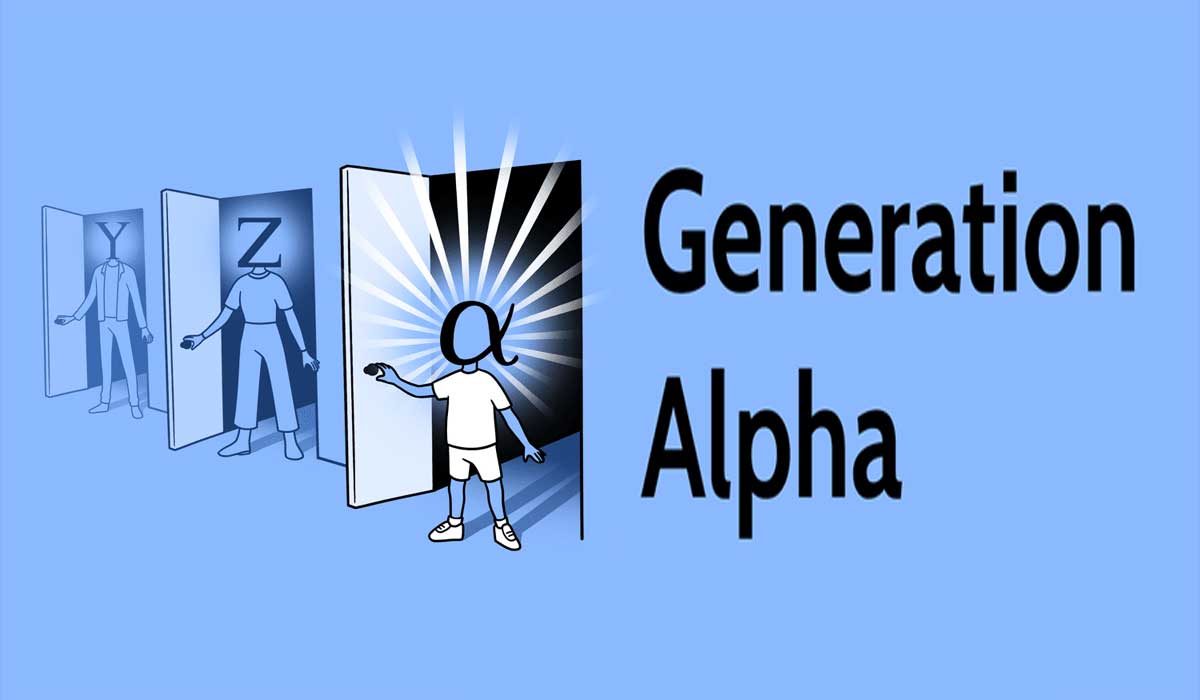
“मुझे नियम पता हैं, कृपया उन्हें समझाना शुरू मत कीजिए।”
आज के बच्चों की आँखों में ज्ञान की नहीं, प्रतिक्रिया की चमक है। वे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमने उन्हें सुना ही नहीं। “मुझे नियम पता हैं, कृपया उन्हें समझाना शुरू मत कीजिए” — यह वाक्य केवल एक बाल संवाद नहीं, बल्कि आधुनिक पालन-पोषण की थकान, असुरक्षा और भावनात्मक दूरी का आईना है। जब बच्चा यह कहता है, वह नियम नहीं, रिश्ते के स्वरूप पर सवाल उठा रहा होता है। यह समय बच्चों को अनुशासन नहीं, संवाद सिखाने का है — वरना आने वाला समाज समझदार तो होगा, पर संवेदनशील नहीं।
डॉ. प्रियंका सौरभ
 जब मैंने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में दस वर्षीय बालक इशित का वह दृश्य देखा जिसमें उसने अमिताभ बच्चन से कहा — “मुझे नियम पता हैं, कृपया उन्हें समझाना शुरू मत कीजिए”, तो मैं तनिक भी अचंभित नहीं हुई। मैंने ऐसे अनेक बालक देखे हैं जिनके शब्दों में आयु से अधिक प्रौढ़ता होती है, पर भावनाओं में बचपन कहीं पीछे छूट जाता है। समाज माध्यमों पर किसी ने उसे घमंडी कहा, किसी ने कहा कि माता–पिता ने संस्कार नहीं दिए। पर सच्चाई इन त्वरित प्रतिक्रियाओं से कहीं अधिक गहरी है। वह बालक दरअसल एक पूरी पीढ़ी का दर्पण था — वह पीढ़ी जिसे हम अल्फ़ा पीढ़ी कहते हैं, सबसे तेज़, सबसे अधीर और सबसे अस्थिर पीढ़ी।
जब मैंने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में दस वर्षीय बालक इशित का वह दृश्य देखा जिसमें उसने अमिताभ बच्चन से कहा — “मुझे नियम पता हैं, कृपया उन्हें समझाना शुरू मत कीजिए”, तो मैं तनिक भी अचंभित नहीं हुई। मैंने ऐसे अनेक बालक देखे हैं जिनके शब्दों में आयु से अधिक प्रौढ़ता होती है, पर भावनाओं में बचपन कहीं पीछे छूट जाता है। समाज माध्यमों पर किसी ने उसे घमंडी कहा, किसी ने कहा कि माता–पिता ने संस्कार नहीं दिए। पर सच्चाई इन त्वरित प्रतिक्रियाओं से कहीं अधिक गहरी है। वह बालक दरअसल एक पूरी पीढ़ी का दर्पण था — वह पीढ़ी जिसे हम अल्फ़ा पीढ़ी कहते हैं, सबसे तेज़, सबसे अधीर और सबसे अस्थिर पीढ़ी।
ये बच्चे उस युग में पल रहे हैं जहाँ हर प्रश्न का उत्तर एक स्पर्श भर की दूरी पर है। इनके बचपन में खेलों की जगह मोबाइल है, साथियों की जगह परदे की चमक है। इन्हें सब कुछ “तुरंत” चाहिए — उत्तर भी, ध्यान भी, प्रशंसा भी। पर इस तात्कालिकता की कीमत चुकानी पड़ रही है। उनके मस्तिष्क का वह भाग, जो धैर्य, निर्णय और भावनाओं का नियंत्रण संभालता है, परिपक्व होने से पहले ही सूचना की बाढ़ में बह जाता है। परिणाम यह कि विचार की गति बहुत तेज़ हो गई है, पर नियंत्रण की क्षमता कमज़ोर होती जा रही है। ये बच्चे जानते बहुत हैं, पर ठहरकर सुनना नहीं जानते। इशित का व्यवहार उसी बेचैनी का प्रतीक था। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, पर उस आत्मविश्वास के पीछे एक छिपा हुआ भय भी था। जिस आयु में बच्चों को प्रश्न पूछने चाहिए, वह उत्तर देने को उतावला था। यह केवल एक बच्चे की प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक स्थिति का संकेत है। यह व्यवहार किसी मानसिक रोग का नहीं, बल्कि असंतुलित विकास का परिणाम है। जब कोई बच्चा हर समय आगे बोलने, अपने को सही सिद्ध करने और ध्यान आकर्षित करने में लगा रहे, तो वह भीतर से किसी अदृश्य दबाव में जी रहा होता है।
Government Advertisement...
अक्सर ऐसे बच्चे किसी अदृश्य प्रतियोगिता में बंधे रहते हैं। वे यह मान लेते हैं कि उन्हें हर हाल में बुद्धिमान और सफल दिखना ही है। उनका यह दिखावटी आत्मविश्वास एक परदे की तरह होता है जिसके पीछे असुरक्षा, डर और प्रदर्शन की चिंता छिपी रहती है। इशित ने जब कहा — “यदि मैं बारह लाख रुपये नहीं जीत पाया तो मुझे आपके साथ चित्र खिंचवाने की अनुमति नहीं होगी”, तब यह स्पष्ट था कि उसके आत्म–मूल्य को उपलब्धि से जोड़ दिया गया है। यह दबाव परिवार, विद्यालय और समाज तीनों की अपेक्षाओं से उपजता है। आज के माता–पिता अपने बच्चों की बुद्धि और जीत की प्रशंसा करते हैं, पर उनकी भावनाओं पर कम ध्यान देते हैं। बच्चों को चतुर बनाना प्राथमिकता है, संयमी बनाना नहीं। यह भूल जाना कि बच्चों की सीखने की सबसे बड़ी शक्ति उनका अनुकरण है। वे हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से सीखते हैं। यदि घर में झुँझलाहट, अधैर्य और कटुता है, तो वही रूप वे समाज में दोहराएँगे। परिवार में जो स्वभाव बीज की तरह बोया जाता है, वही समाज में वृक्ष बनकर उगता है।
विद्यालयों में भी यही दृश्य है। सातवीं कक्षा का विद्यार्थी कहता है — “मुझे सब कुछ पहले से ज्ञात है।” आठवीं की छात्रा समाज माध्यमों पर मिले प्रेम और लोकप्रियता के जाल में उलझकर टूट जाती है। यह केवल अभिभावकों की भूल नहीं, बल्कि उस शिक्षा प्रणाली की भी है जो हर बालक से एक समान गति और परिणाम की अपेक्षा रखती है। जो बच्चा उस साँचे में फिट नहीं बैठता, वह विद्रोही कहलाता है। कभी–कभी उसका विद्रोह केवल अपनी असंगति का स्वर होता है, अपराध नहीं। हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हमने ज्ञान को तेज़ी का पर्याय बना दिया है। तकनीकी निपुणता को परिपक्वता समझ लिया है। पर असली संकट यह है कि हमारी नई पीढ़ी भावनात्मक रूप से अस्थिर होती जा रही है। वह बाहर की दुनिया से तो संवाद करती है, पर अपने भीतर से नहीं। विद्यालय, उपकरण और समाज की स्पर्धा ने बच्चों से बचपन का ठहराव छीन लिया है। अब जो बच्चा शांत है, उसे “धीमा” कहा जाता है, और जो शोर करता है वही “सफल” कहलाता है। यही हमारी सभ्यता का उलटापन है।
समस्या बच्चे में नहीं, हमारी दृष्टि में है। हमने बच्चों को बोलना सिखाया, पर सुनना नहीं; ज्ञान दिया, पर संवेदना नहीं। हमने उन्हें उपलब्धि का पाठ पढ़ाया, पर संतुलन का नहीं। इसीलिए आज जो बच्चा अपनी भावना व्यक्त करता है, उसे तुरंत दोषी ठहरा दिया जाता है — “संस्कारहीन”, “घमंडी”, “बाग़ी।” पर वह बच्चा केवल हमारी अपनी अधीरता का प्रतिबिंब है। हमारे घर, हमारे विद्यालय और हमारा समाज मिलकर उस मासूम मन को एक मशीन में बदल रहे हैं जो बोलता तो बहुत है पर समझता कम है। अब शिक्षा में प्रतियोगिता है, पालन–पोषण में प्रदर्शन है और समाज में तुलना है। इन तीनों ने मिलकर बच्चे के मन से उसकी सहजता छीन ली है। अब आवश्यकता है सोच और प्रणाली दोनों को बदलने की। बच्चों को केवल ज्ञान नहीं, संवेदना की शिक्षा चाहिए। उन्हें जीतना नहीं, ठहरना सिखाना होगा। यदि हमने यह दिशा नहीं बदली तो विनम्रता और धैर्य जैसे गुणों को ही असामान्यता कहा जाएगा। समाज उस ओर बढ़ रहा है जहाँ शांत व्यक्ति को कमजोर माना जाएगा और चिल्लाने वाले को सफल। यह वह खतरनाक दौर है जहाँ सभ्यता की जड़ें सूखने लगती हैं।
विडंबना यह भी है कि जिन वयस्कों ने उस बालक की आलोचना की, वे स्वयं समाज माध्यमों पर गुस्सा, असम्मान और अपशब्दों की भाषा बोलते हैं। जो पीढ़ी स्वयं संयम खो चुकी है, वह बच्चों को मर्यादा कैसे सिखा सकती है? यही सबसे गहरी चिंता है। वह बालक दोष नहीं, संकेत है। वह हमें यह दिखाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम तकनीकी रूप से निपुण, पर मानसिक रूप से थके हुए नागरिक गढ़ रहे हैं। वह बालक हमारे भीतर की हड़बड़ी, हमारी अपेक्षाओं और हमारे असंतुलन का आईना है। उसे डाँटने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। हर अति–चतुर बच्चे के भीतर एक उज्ज्वल परंतु डरा हुआ मन छिपा है, जिसे दबाने की नहीं, दिशा देने की ज़रूरत है। जब तक हम बच्चों को उपलब्धि से अधिक संवेदना, और बुद्धि से अधिक विनम्रता का पाठ नहीं पढ़ाएँगे, तब तक वे हमारी अधूरी आकांक्षाओं के बोझ तले पलते रहेंगे। वह बालक दरअसल हमारा ही प्रतिबिंब था — और शायद अब डर हमें उस प्रतिबिंब से होना चाहिए, जिससे हम मुँह फेरते जा रहे हैं।
डॉ. प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर (राजनीतिशास्त्र), कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)















