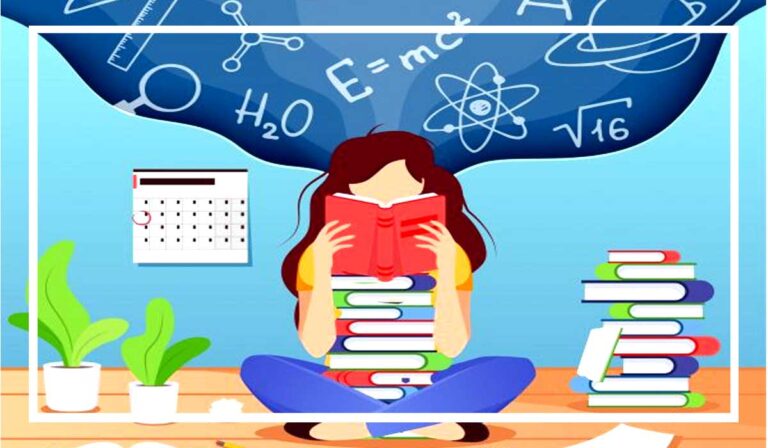यह आलेख कोचिंग संस्कृति और प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव के कारण बढ़ती छात्र आत्महत्याओं पर गंभीर प्रश्न उठाता है। कृति के सुसाइड नोट के संदर्भ में लेखक सफलता की संकीर्ण परिभाषा, माता-पिता की अपेक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था की खामियों की पड़ताल करता है। लेख समाज, सरकार और कोचिंग उद्योग से संवेदनशील और ठोस बदलाव की मांग करता है।
- कोचिंग संस्कृति का काला सच
- रैंक के दबाव में टूटती ज़िंदगियाँ
- सपनों का बोझ और बच्चों की चुप्पी
- चयन की होड़, संवेदना की हार
डॉ. प्रियंका सौरभ
 कोटा में एक और छात्रा की आत्महत्या—यह कोई साधारण खबर नहीं है और न ही किसी एक परिवार की निजी त्रासदी भर। यह उस शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक मानसिकता और तथाकथित “सफलता मॉडल” पर गहरा प्रश्नचिह्न है, जिसे हमने पिछले दो दशकों में बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है। आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति का सुसाइड नोट केवल व्यक्तिगत पीड़ा का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि वह एक आरोपपत्र की तरह हमारे पूरे समाज के सामने खड़ा होता है—माता-पिता, कोचिंग संस्थान, स्कूल और नीति-निर्माता सभी इसके दायरे में आते हैं। कृति ने अपने सुसाइड नोट में भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से अपील की थी कि अगर वे सच में चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे, तो कोचिंग संस्थानों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान छात्रों को भीतर से खोखला कर देते हैं।
कोटा में एक और छात्रा की आत्महत्या—यह कोई साधारण खबर नहीं है और न ही किसी एक परिवार की निजी त्रासदी भर। यह उस शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक मानसिकता और तथाकथित “सफलता मॉडल” पर गहरा प्रश्नचिह्न है, जिसे हमने पिछले दो दशकों में बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है। आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति का सुसाइड नोट केवल व्यक्तिगत पीड़ा का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि वह एक आरोपपत्र की तरह हमारे पूरे समाज के सामने खड़ा होता है—माता-पिता, कोचिंग संस्थान, स्कूल और नीति-निर्माता सभी इसके दायरे में आते हैं। कृति ने अपने सुसाइड नोट में भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से अपील की थी कि अगर वे सच में चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे, तो कोचिंग संस्थानों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान छात्रों को भीतर से खोखला कर देते हैं।
Government Advertisement...
यह कथन किसी क्षणिक आवेग का परिणाम नहीं था, बल्कि उस लंबे मानसिक उत्पीड़न की अभिव्यक्ति थी, जिसे आज लाखों छात्र रोज़ झेल रहे हैं। असली सवाल यह नहीं है कि कृति ने ऐसा क्यों लिखा, बल्कि यह है कि क्या वह ग़लत थी। आज भारत में कोचिंग शिक्षा का सहायक माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि एक विशाल और मुनाफ़े पर आधारित उद्योग बन चुकी है। कोटा, सीकर, हैदराबाद, दिल्ली और पटना जैसे शहर “एजुकेशन हब” कहलाते हैं, जहाँ हर साल लाखों किशोर अपने माता-पिता के सपनों का बोझ उठाए पहुँचते हैं। इन सपनों के केंद्र में कुछ सीमित शब्द होते हैं—आईआईटी, एम्स, नीट, रैंक और सेलेक्शन। कोचिंग संस्थान बच्चों को यह यक़ीन दिलाते हैं कि यदि वे चयनित नहीं हुए, तो वे असफल हैं। सफलता की यह परिभाषा इतनी संकीर्ण है कि उसमें औसत छात्र के लिए कोई जगह नहीं बचती, और असफलता से उबरने की कोई मानवीय प्रक्रिया भी नहीं होती।
कृति का यह कथन कि “90+ अंक लाने वाली लड़की भी आत्महत्या कर सकती है” हमारे उस भ्रम को तोड़ता है, जिसमें हम यह मान लेते हैं कि मानसिक संकट केवल कमजोर या असफल छात्रों तक सीमित है। यह सोच न सिर्फ़ ग़लत है, बल्कि ख़तरनाक भी है। आज का दबाव केवल परीक्षा पास करने या अच्छे अंक लाने का नहीं रह गया है, बल्कि माता-पिता, शिक्षकों और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का बन गया है। हर बच्चा अपने भीतर एक काल्पनिक ‘परफेक्ट स्टूडेंट’ की छवि ढो रहा है, जिससे वह लगातार हारता चला जाता है। ऊँचे अंक और बेहतर प्रदर्शन भी अब मानसिक शांति की गारंटी नहीं रहे, क्योंकि समस्या पढ़ाई की नहीं, बल्कि उस माहौल की है जिसमें पढ़ाई कराई जा रही है।
कृति द्वारा अपनी माँ के लिए लिखी गई पंक्तियाँ इस पूरे संकट की जड़ को उजागर करती हैं। वह बताती है कि उसे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसकी वास्तविक रुचि अंग्रेज़ी साहित्य और इतिहास में थी। यह कहानी किसी एक घर तक सीमित नहीं है। यह देश के हज़ारों, बल्कि लाखों घरों की सच्चाई है, जहाँ बच्चे की रुचि से ज़्यादा समाज की अपेक्षा मायने रखती है। माता-पिता अक्सर यह भूल जाते हैं कि बच्चा उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। सामाजिक तुलना—कि फलाँ का बेटा डॉक्टर बन गया या फलाँ की बेटी आईआईटी में पहुँच गई—हमें इतना अंधा कर देती है कि हम बच्चों की इच्छाओं, क्षमताओं और सीमाओं को अनदेखा कर देते हैं।
कृति ने अपनी छोटी बहन को लेकर जो चेतावनी दी, वह इस सुसाइड नोट को और भी मार्मिक बना देती है। वह चाहती है कि उसकी बहन को वही पढ़ने दिया जाए, जो वह पढ़ना चाहती है, और वही बनने दिया जाए, जो वह बनना चाहती है। यह विडंबना है कि मरते समय भी वह किसी और की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। यह चेतावनी केवल एक माँ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है, जो बच्चों को सुनने के बजाय उन पर अपने सपने थोपता है। आज के स्कूल और कोचिंग संस्थान बच्चों को गणित के सूत्र, रसायन के समीकरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीतियाँ तो सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन के सबसे ज़रूरी पाठ सिखाने में पूरी तरह असफल हो रहे हैं। वे बच्चों को यह नहीं सिखा पा रहे कि असफलता से कैसे निपटना है, मानसिक तनाव को कैसे समझना है और मदद माँगना कमजोरी नहीं है। प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा के बजाय भय का औज़ार बना दिया गया है। रैंक लिस्ट, मॉक टेस्ट और लगातार तुलना बच्चों के मन में स्थायी हीनभावना भर देती है, जिससे वे खुद को केवल अंकों और चयन के चश्मे से देखने लगते हैं।
हर ऐसी मौत के बाद सरकार की ओर से औपचारिक बयान आते हैं, जाँच के आदेश दिए जाते हैं और कुछ दिनों तक बहस चलती है। इसके बाद सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। न कोचिंग संस्थानों के कामकाज पर सख्त निगरानी होती है, न उनके घंटे सीमित किए जाते हैं, न मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाता है। यदि सरकार सच में गंभीर है, तो कोचिंग उद्योग के लिए सख्त नियमन, छात्रों के लिए सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सहायता और स्कूल स्तर पर करियर की विविध संभावनाओं को स्वीकार करने की ठोस नीति बनानी होगी।
सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम सफलता को किस रूप में परिभाषित करते हैं। क्या एक अच्छा इंसान बनना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और अपनी रुचि के क्षेत्र में संतुष्ट जीवन जीना सफलता नहीं है? यदि नहीं, तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो चयनित तो होगी, लेकिन भीतर से टूटी हुई और असंतुष्ट होगी। कृति की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम अपने बच्चों को ज़िंदा रहते हुए ही तो नहीं मार रहे—उनकी इच्छाओं को, उनके सपनों को और उनकी स्वतंत्रता को। कृति का सुसाइड नोट केवल एक छात्रा की अंतिम अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। अगर अब भी हमने नहीं सुना, नहीं समझा और नहीं बदले, तो ऐसी घटनाएँ रुकने वाली नहीं हैं। सवाल यह नहीं है कि अगला बच्चा कौन होगा। असली सवाल यह है कि क्या हम अगले बच्चे को बचा पाएँगे।
(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)
डॉ. प्रियंका सौरभ
पीएचडी (राजनीति विज्ञान)
कवयित्री | सामाजिक चिंतक | स्तंभकार, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)