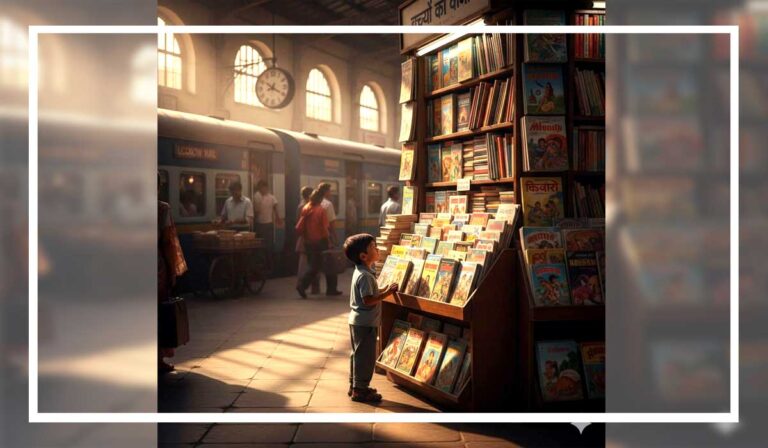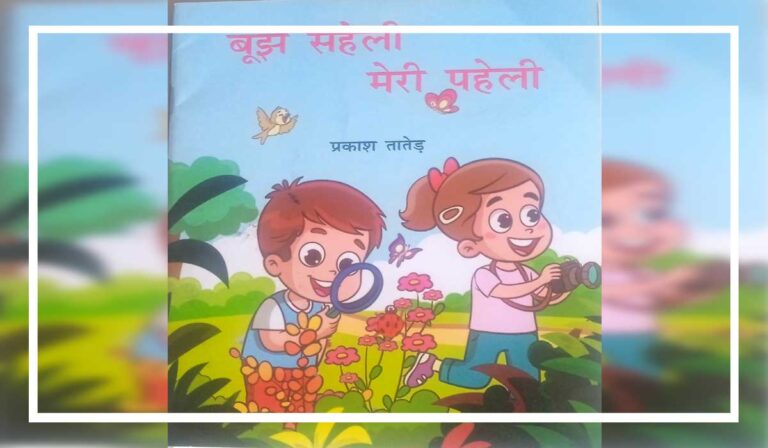यह आलेख देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बढ़ती मुनाफ़ाख़ोरी, निजी अस्पतालों की लूट और इंश्योरेंस के दुरुपयोग को उजागर करता है। लेखिका बताती हैं कि कैसे आम आदमी बीमारी से ज़्यादा इलाज के बिल से डरने लगा है और सरकारी व्यवस्था की कमजोरी इस शोषण को बढ़ावा दे रही है।
- मुनाफ़े का कारोबार बनता इलाज
- इंश्योरेंस और अस्पतालों का खतरनाक गठजोड़
- सरकारी व्यवस्था की कमजोरी, निजी लूट की ताक़त
- इलाज से उठता भरोसा, बीमार होती व्यवस्था
डॉ. प्रियंका सौरभ
 आज देश की हॉस्पिटल व्यवस्था जिस हालत में पहुँच चुकी है, वह किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों आम नागरिकों का साझा अनुभव बनती जा रही है। इलाज, जो कभी सेवा और संवेदना का क्षेत्र माना जाता था, अब धीरे-धीरे मुनाफ़े का ऐसा संगठित उद्योग बन चुका है, जहाँ इंसान की बीमारी से ज़्यादा उसकी जेब, उसका इंश्योरेंस और उसका सामाजिक दर्जा देखा जाता है। बड़े-बड़े निजी अस्पतालों की चमक-दमक, एयर-कंडीशन्ड गलियारे और आधुनिक मशीनें बाहर से भले ही तरक्की का भ्रम पैदा करती हों, लेकिन भीतर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, जो आम आदमी के लिए किसी आर्थिक यातना से कम नहीं है।
आज देश की हॉस्पिटल व्यवस्था जिस हालत में पहुँच चुकी है, वह किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों आम नागरिकों का साझा अनुभव बनती जा रही है। इलाज, जो कभी सेवा और संवेदना का क्षेत्र माना जाता था, अब धीरे-धीरे मुनाफ़े का ऐसा संगठित उद्योग बन चुका है, जहाँ इंसान की बीमारी से ज़्यादा उसकी जेब, उसका इंश्योरेंस और उसका सामाजिक दर्जा देखा जाता है। बड़े-बड़े निजी अस्पतालों की चमक-दमक, एयर-कंडीशन्ड गलियारे और आधुनिक मशीनें बाहर से भले ही तरक्की का भ्रम पैदा करती हों, लेकिन भीतर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, जो आम आदमी के लिए किसी आर्थिक यातना से कम नहीं है।
Government Advertisement...
आज अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने जाता है, तो सबसे पहला सवाल उसकी बीमारी को लेकर नहीं, बल्कि उसकी भुगतान क्षमता को लेकर होता है। रिसेप्शन पर, एडमिशन काउंटर पर या डॉक्टर से मिलने से पहले ही यह पूछा जाता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट, कैश में भुगतान करेंगे या कैशलेस। इस एक सवाल के जवाब से मरीज का पूरा इलाज तय हो जाता है। जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि मरीज इंश्योरेंस कवर में है या किसी सरकारी/कॉर्पोरेट स्कीम के अंतर्गत आता है, अस्पताल का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। इलाज की जगह एक योजनाबद्ध कमाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
इंश्योरेंस होने का मतलब होना चाहिए सुरक्षा, लेकिन आज के समय में यह कई निजी अस्पतालों के लिए खुली छूट का लाइसेंस बन चुका है। ज़रूरत से ज़्यादा महँगी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, जिनके सस्ते और समान प्रभाव वाले विकल्प आसानी से उपलब्ध होते हैं। ऐसे-ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं, जिनका न तो बीमारी से सीधा संबंध होता है और न ही इलाज की दिशा तय करने में कोई ठोस भूमिका। एमआरआई, सीटी स्कैन, बार-बार की ब्लड जाँच, स्पेशल पैनल टेस्ट—सब कुछ “रूटीन” के नाम पर जोड़ दिया जाता है। मरीज और उसके परिजन डॉक्टर की बात पर आँख मूँदकर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर उनके भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, जबकि हकीकत कई बार इससे उलट होती है।
सबसे चिंताजनक स्थिति तब बनती है, जब मरीज की हालत में सुधार हो जाने के बावजूद उसे अस्पताल में रोके रखा जाता है। जो मरीज सामान्य परिस्थितियों में चार-पाँच दिन में डिस्चार्ज हो सकता है, उसे जानबूझकर दस-पंद्रह दिन तक भर्ती रखा जाता है। कारण साफ़ है—जितने ज़्यादा दिन भर्ती, उतना ज़्यादा बिल। बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विज़िट, दवाइयाँ, कंज़्यूमेबल्स—हर दिन के साथ बिल फूलता चला जाता है। मरीज की सेहत से ज़्यादा ध्यान अब इस बात पर होता है कि इंश्योरेंस क्लेम की सीमा पूरी तरह इस्तेमाल हो जाए।
इस पूरी प्रक्रिया में आम आदमी सबसे ज़्यादा असहाय होता है। उसे न तो मेडिकल ज्ञान होता है और न ही अस्पताल की जटिल बिलिंग प्रणाली को समझने की क्षमता। अगर कोई सवाल करता है, तो उसे डराया जाता है कि इलाज प्रभावित हो सकता है, या फिर तकनीकी शब्दों में ऐसा उलझा दिया जाता है कि वह चुप रह जाना ही बेहतर समझता है। कई बार मरीज के परिजन यह भी महसूस करते हैं कि उन्हें जानबूझकर भ्रम में रखा जा रहा है, लेकिन बीमार व्यक्ति की जान दाँव पर लगी हो, तो विरोध करने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं।
सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। वहाँ इलाज सस्ता या मुफ्त तो है, लेकिन भीड़, संसाधनों की कमी और अव्यवस्था के कारण मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बेड की कमी, स्टाफ की कमी और दवाइयों की अनुपलब्धता के चलते कई लोग मजबूरी में निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। इस मजबूरी का फायदा निजी अस्पताल बखूबी उठाते हैं। एक तरह से सरकारी व्यवस्था की कमजोरी, निजी लूट को और मज़बूत कर रही है।
स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ, जिनका उद्देश्य आम आदमी को आर्थिक सुरक्षा देना था, आज कई मामलों में उल्टा असर डाल रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियाँ और अस्पतालों के बीच एक अघोषित गठजोड़ सा दिखाई देता है, जिसमें मरीज सिर्फ़ एक माध्यम बनकर रह जाता है। फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए बिल, अनावश्यक प्रक्रियाएँ और पैकेज सिस्टम के नाम पर तयशुदा लूट—ये सब अब अपवाद नहीं, बल्कि आम चलन बनते जा रहे हैं। दुखद यह है कि इस पूरे खेल में नैतिकता कहीं पीछे छूट जाती है।
यह भी देखने में आता है कि एक ही बीमारी के इलाज का खर्च अलग-अलग मरीजों के लिए अलग-अलग होता है। जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, उसके लिए इलाज “कम खर्च” में समेट दिया जाता है और जिसके पास इंश्योरेंस है, उसके लिए वही बीमारी कई गुना महँगी हो जाती है। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? बीमारी तो एक-सी है, इलाज भी लगभग वही है, लेकिन बिल में ज़मीन-आसमान का अंतर सिर्फ़ भुगतान के स्रोत के कारण। इस स्थिति का सबसे भयावह पहलू यह है कि धीरे-धीरे लोगों का चिकित्सा व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। डॉक्टर, जिन्हें कभी भगवान का दर्जा दिया जाता था, अब शक की नज़र से देखे जाने लगे हैं। हर पर्ची, हर टेस्ट और हर सलाह पर सवाल उठने लगा है कि यह ज़रूरी है या सिर्फ़ कमाई का ज़रिया। यह अविश्वास पूरे समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकती।
सरकार की ज़िम्मेदारी यहाँ बेहद अहम हो जाती है। स्वास्थ्य को सिर्फ़ बाज़ार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सख़्त रेगुलेशन, पारदर्शी बिलिंग सिस्टम और प्रभावी निगरानी के बिना निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाना मुश्किल है। इलाज की दरों, बेड चार्ज, टेस्ट और दवाइयों की कीमतों पर स्पष्ट और कड़ाई से लागू होने वाले नियम होने चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया में स्वतंत्र ऑडिट और शिकायत निवारण की मज़बूत व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि मरीज को न्याय मिल सके। इसके साथ-साथ सरकारी अस्पतालों को मज़बूत करना भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक आम आदमी को भरोसेमंद, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिलेंगी, तब तक वह निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होता रहेगा। स्वास्थ्य को खर्च नहीं, बल्कि निवेश मानकर देखना होगा—निवेश, जो देश की सबसे बड़ी पूंजी, यानी उसके नागरिकों के जीवन में किया जाता है।
आख़िर में सवाल सिर्फ़ व्यवस्था का नहीं, बल्कि सोच का भी है। क्या हम इलाज को सिर्फ़ मुनाफ़े का साधन मानने को तैयार हैं, या फिर उसे इंसानियत और सेवा से जोड़कर देखना चाहते हैं? अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वह दिन दूर नहीं जब बीमारी से ज़्यादा डर इलाज के बिल से लगने लगेगा। और जब इलाज डर का कारण बन जाए, तब समझ लेना चाहिए कि व्यवस्था गंभीर रूप से बीमार हो चुकी है—और उसका इलाज अब टालना, पूरे समाज के लिए घातक साबित हो सकता है।
(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)
डॉ. प्रियंका सौरभ
पीएचडी (राजनीति विज्ञान) कवयित्री | सामाजिक चिंतक | स्तंभकार उब्बा भवन, आर्यनगर हिसार (हरियाणा)