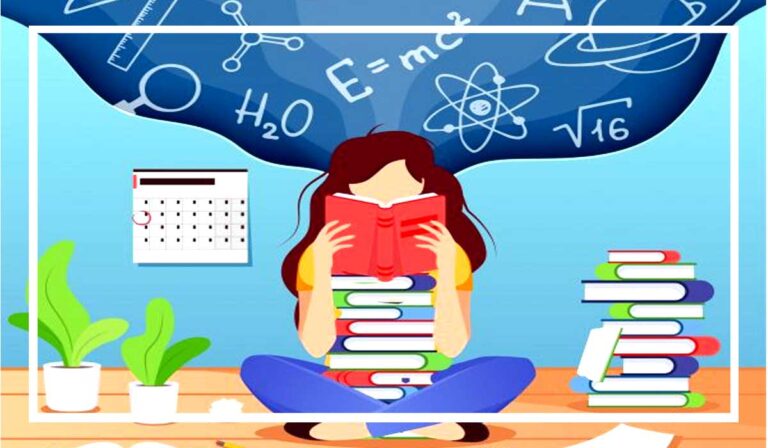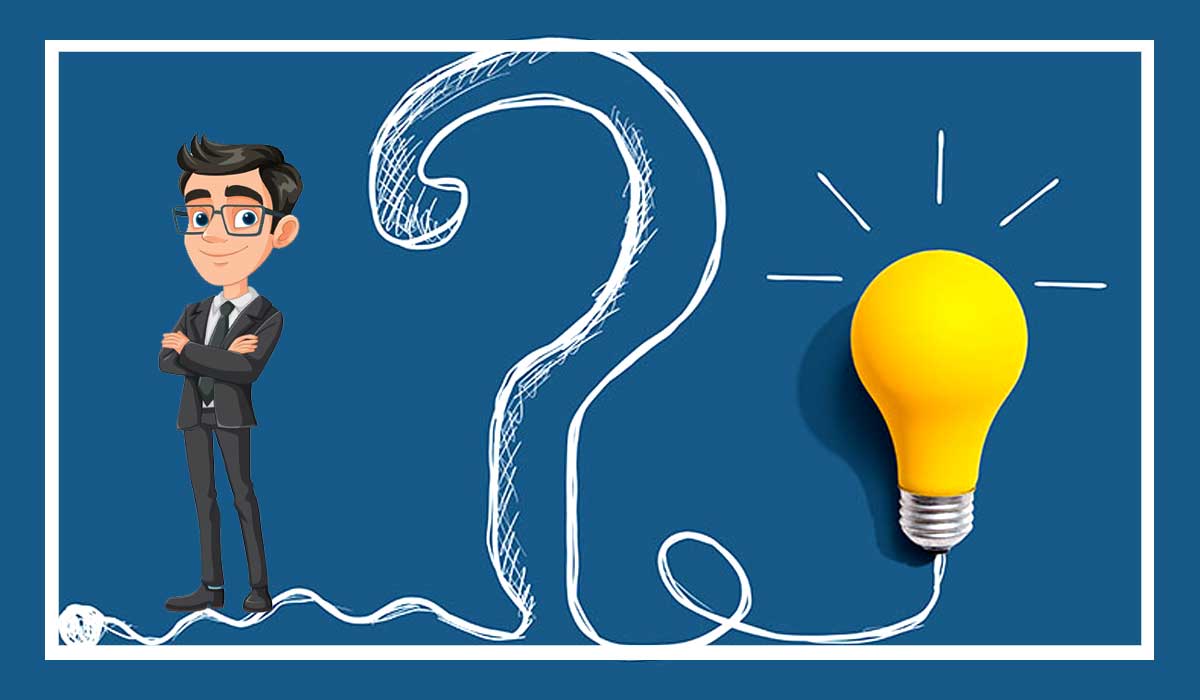
यह कविता उस श्रमिक वर्ग की मौन पीड़ा को सामने लाती है जो विकास के शोर में अदृश्य बना रहता है। रचना में एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण है जिसकी पहचान केवल उसके काम तक सीमित है और जो सिस्टम के भीतर धीरे-धीरे गायब होता जाता है। कविता यथार्थ, विस्थापन, श्रम, भय और टूटती उम्मीदों का सघन सामाजिक दस्तावेज़ बनकर उभरती है।
- विकास के शोर में दबा एक आदमी
- काम खत्म होता है, आदमी नहीं
- शहर, मशीन और पीछे छूटता जीवन
- आँकड़ों में नहीं दर्ज होती थकान
शिवम यादव अन्तापुरिया
कानपुर उत्तर प्रदेश
Government Advertisement...
मैं नहीं देखना चाहता
चमकते शहरों के ऊपर उड़ते ड्रोन
जो हर गली को माप लेते हैं
पर किसी भूखे की आँख की नमी दर्ज नहीं करते
मैं देखना चाहता हूँ
दोपहर की धूप में ठिठकी हुई एक औरत
जिसके हाथ में राशन की पर्ची है
और दिमाग़ में हिसाब—
कि आज बच्चे को पूरा खिलाए
या कल के लिए थोड़ा बचा ले
मैं नहीं समझना चाहता
विकास के ग्राफ़
जो ऊपर चढ़ते हैं
जब नीचे लोग गायब हो जाते हैं
मैं समझना चाहता हूँ
उस खामोशी को
जो तब पैदा होती है
जब कोई मज़दूर
अपने गाँव लौटते समय
स्टेशन पर आख़िरी बार पीछे मुड़कर देखता है
और जानता है
कि यह लौटना नहीं है—
बस एक और विस्थापन है
मुझे नहीं चाहिए
उपदेश, प्रेरक वाक्य,
“सब ठीक हो जाएगा” की झूठी पट्टियाँ
मुझे चाहिए
रात के तीन बजे
फैक्ट्री के बाहर खड़े चौकीदार की उनींदी आँखें
जिनमें पूरा देश पहरा दे रहा है
और फिर भी असुरक्षित है
मैं सुनना चाहता हूँ
उन चप्पलों की आवाज़
जो हर सुबह जल्दी-जल्दी चलती हैं
क्योंकि देर हो जाने का मतलब
सिर्फ़ डाँट नहीं
भूख भी हो सकता है
और अगर यह सब पढ़ना
किसी को भारी लगे
तो लगे—
क्योंकि जिन पर बीतती है
उनके लिए यह कविता नहीं
दैनिक जीवन है
अब कोई रूपक नहीं बचाते।
सिर्फ़ जो है, वही।
एक आदमी है
वह रोज़ काम पर जाता है
काम खत्म हो जाता है
वह नहीं
उसके हाथों में छाले हैं
डिग्री नहीं
इसलिए उसकी थकान
किसी रिपोर्ट में नहीं आती
वह खाता है
ताकि मर न जाए
और जीता है
ताकि कल फिर खा सके
उसकी पत्नी पूछती नहीं
“कैसा रहा दिन”
वह पूछती है
“पैसे पूरे हैं?”
बच्चा रोता है
क्योंकि बच्चा है
बाप चुप रहता है
क्योंकि बाप है
शहर उसे जानता नहीं
बस इस्तेमाल करता है
जब वह बीमार पड़ता है
तो छुट्टी नहीं लेता
क्योंकि बीमारी
उसकी है
नुकसान कंपनी का होगा
एक दिन वह नहीं आएगा
कोई नोटिस नहीं लगेगा
दूसरा आदमी आ जाएगा
फर्श वही रहेगा
मशीन वही रहेगी
देश आगे बढ़ता रहेगा
और कहीं कोई कहेगा—
“रोज़गार पैदा हो रहा है”
फ़िर से जब
वह घर लौटता है
दरवाज़ा खोलने से पहले
जेब टटोलता है
जैसे जेब
उसकी इज़्ज़त हो
घर छोटा है
पर आवाज़ें कम नहीं
बर्तन बोलते हैं
बिजली का बिल
दीवार पर टँगा
मुँह खोलकर खड़ा है
वह टीवी नहीं देखता
क्योंकि उसमें
उस जैसा कोई नहीं
और अगर है भी
तो उसे
“प्रेरणा” कहा जाता है
रविवार को
वह देर तक सोना चाहता है
पर नींद
ओवरटाइम नहीं करती
उसका सपना था
कभी नहीं पूछा गया
अब उसकी याद भी
महीने के आख़िर तक
नहीं टिकती
वह लाइन में खड़ा होता है
राशन के लिए
बस के लिए
ज़िंदगी के लिए
हर लाइन में
वह पीछे ही रहता है
जब वह हँसता है
तो थोड़ा सा
माफ़ी माँगता है
जैसे हँसी
उसके पद से बाहर हो
वह जानता है
अगर वह टूटेगा
तो खबर नहीं बनेगा
बस आँकड़ा बदलेगा
और एक दिन
उसका बच्चा बड़ा होकर
उस जैसा ही काम करेगा
फर्क सिर्फ़ इतना होगा—
मशीन नई होगी
और उम्मीद
और पुरानी
देश तब भी कहेगा—
“हम आगे बढ़ रहे हैं”
वह आदमी
तब भी
पीछे खड़ा होगा
वह आदमी
अपने नाम से नहीं पहचाना जाता
उसे पहचाना जाता है
उसके काम से
और काम ख़त्म होते ही
उसकी पहचान भी
उसके काग़ज़ों में
एक नंबर है
जो कभी
उसकी आवाज़ नहीं बना
बस साबित करता रहा
कि वह मौजूद है
वह चुप रहना सीख गया है
क्योंकि बोलने से
कुछ बदलता नहीं
और चुप रहने से
कम से कम
नौकरी तो रहती है
जब कोई मरता है
उसकी बस्ती में
तो वह रोता नहीं
क्योंकि रोना
छुट्टी में नहीं गिना जाता
उसकी पीठ झुकी नहीं
ढाली गई है
धीरे-धीरे
रोज़
जैसे सिस्टम
अपनी शक्ल
उसके शरीर में उतार रहा हो
वह भगवान को
याद नहीं करता
क्योंकि भगवान
समय माँगते हैं
और उसके पास
सिर्फ़ काम है
वह जानता है
कि कानून किताबों में है
और किताबें
उसके हाथों में
कभी नहीं आईं
जब वह बूढ़ा होगा
तो उसे
“अनुपयोगी” कहा जाएगा
और वह पहली बार
किसी शब्द में
पूरी तरह फिट बैठेगा
उस दिन
उसके औज़ार
किसी और को दे दिए जाएँगे
और उसकी आदतें
किसी को नहीं
उसकी मौत
शायद घर में होगी
या किसी बस में
या काम पर
फर्क़ नहीं पड़ेगा
क्योंकि किसी जगह
उसके लिए
जगह थी ही नहीं
और जब सब हो जाएगा
तो एक फ़ाइल बंद होगी
बिना पढ़े
फिर वही शहर
वही मशीन
वही नारा
और कहीं
कोई फिर कहेगा—
“मेहनत से
सब कुछ बदला जा सकता है”
वह आदमी
तब भी
उदाहरण नहीं बनेगा
उसके भीतर
कोई चीख़ नहीं
क्योंकि चीख़
उम्मीद माँगती है
और उम्मीद
वह बहुत पहले
खर्च कर चुका
उसके भीतर
एक लगातार चलता हिसाब है—
कितना सह लिया
कितना बचा
और कितना
कल के लिए
टाल दिया
वह अपने डर को
नाम नहीं देता
क्योंकि नाम देने से
वह सच हो जाता है
इसलिए डर
बस आदत बनकर
उसके साथ रहता है
उसके भीतर
थकान नहीं है
थकान तो बाहर दिखती है
भीतर है
एक खालीपन
जो हर सुबह
काम पर निकलते समय
ठीक से बंद नहीं होता
कभी-कभी
उसे लगता है
अगर वह रुक गया
तो सब गिर जाएगा
घर
बच्चा
दिन
इसलिए वह चलता रहता है
जैसे रुकना
उसकी ज़िम्मेदारी नहीं
कोई अपराध हो
उसके भीतर
एक आवाज़ है
जो पूछती है—
“क्या यह सब ज़रूरी था?”
वह उस आवाज़ को
भूख से दबा देता है
वह जानता है
कि वह बदला नहीं जाएगा
इसलिए उसने
अपने भीतर
लड़ना छोड़ दिया है
अब वह
खुद को संभालता है
जैसे कोई
टूटी चीज़
जो अभी काम आ रही हो
कभी रात में
जब सब सो जाते हैं
तो वह जागता है
इसलिए नहीं कि
सो नहीं पाता
बल्कि इसलिए कि
सोते हुए
उसका होना
किसी काम का नहीं
उसके भीतर
कोई सपना नहीं
सिर्फ़ एक डर है—
कि कल
वह कम पड़ जाएगा
और यही डर
उसे हर सुबह
उठा देता है
बिना सवाल
बिना शिकायत
भीतर उतरने पर
यही मिलता है—
कोई कहानी नहीं
कोई नायक नहीं
बस एक आदमी
जो खुद से
थोड़ा-थोड़ा
गायब होता जा रहा है
और फिर भी
कल
काम पर जाएगा