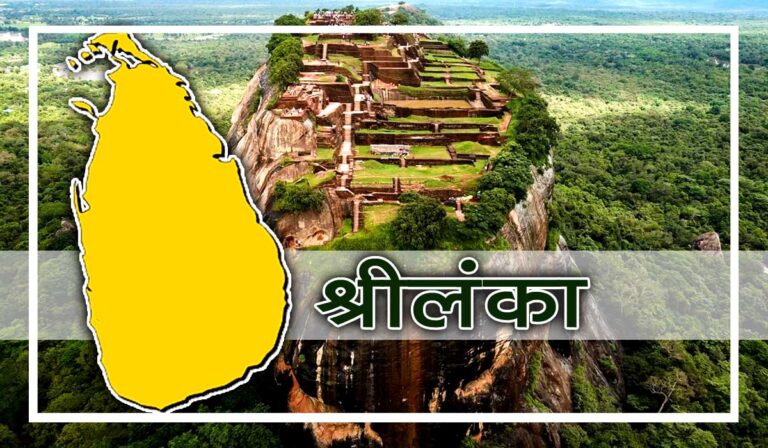सत्येन्द्र कुमार पाठक
 भारतीय चिंतन परंपरा में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्य और आत्म-अभिव्यक्ति का साधन है। यह आलेख भारतीय साहित्य और व्याकरण के आधारभूत स्तंभों—अक्षर, शब्द, वाक्य और ग्रंथ—के महत्व का विशेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इन चारों तत्वों का क्रमिक विकास किस प्रकार साहित्य के विशाल भवन का निर्माण करता है, इसे प्राकृत, संस्कृत और भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के आलोक में समझा जाएगा।
भारतीय चिंतन परंपरा में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्य और आत्म-अभिव्यक्ति का साधन है। यह आलेख भारतीय साहित्य और व्याकरण के आधारभूत स्तंभों—अक्षर, शब्द, वाक्य और ग्रंथ—के महत्व का विशेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इन चारों तत्वों का क्रमिक विकास किस प्रकार साहित्य के विशाल भवन का निर्माण करता है, इसे प्राकृत, संस्कृत और भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के आलोक में समझा जाएगा।
अक्षर: ध्वनि, सत्ता और मंत्र – ‘अक्षर’ का अर्थ है जो नष्ट न हो (अ+क्षर)। यह ध्वनि की अविनाशी इकाई है। भारतीय दर्शन इसे ‘नाद’ या ‘परम-तत्व’ से जोड़ता है। प्राकृत, जो कि संस्कृत की अपेक्षा अधिक सहज और लोक-सुलभ भाषा थी, ने अक्षरों को स्थानीय और व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इस सरलता ने आगे चलकर भाषाओं के विकास की नींव रखी। अक्षर और मंत्र: यह माना गया है कि अक्षर ही मंत्र है। जैसे ‘ॐ’ (प्रणव) एक अक्षर है जो समस्त सृष्टि का बीज है।
Government Advertisement...
प्रत्येक अक्षर में एक शक्ति (बीजाक्षर) निहित है, जो उसका उच्चारण करने वाले को प्रभावित करती है। भारतीय चिंतन परंपरा में भाषा—अक्षर, शब्द, वाक्य और ग्रंथ—केवल संप्रेषण के उपकरण नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्य और ज्ञान के संरक्षण के वाहक हैं। प्रस्तुत आलेख, भारतीय साहित्य और व्याकरण के महान आचार्यों—पतंजलि, राजशेखर, मम्मट भट्ट और विश्वनाथ—के सिद्धांतों के आलोक में इन चारों तत्वों के दार्शनिक आधार और काव्यशास्त्रीय महत्व का विशेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन करता है।
अक्षर: अविनाशी बीज और शब्द-ब्रह्म का प्रथम सोपान – ‘अक्षर’ (अ+क्षर) का शाब्दिक अर्थ है अविनाशी। यह ध्वनि की वह मूलभूत और सूक्ष्म इकाई है जिसे भारतीय दर्शन में परम-तत्व के तुल्य माना गया है। अक्षर ही मंत्र है, और मंत्र ही शब्द-शक्ति का उद्गम है। महर्षि पतंजलि ने अपने ‘व्याकरण महाभाष्य’ में अक्षर की शुद्धता को संरक्षण का मुख्य लक्ष्य माना। शब्द-ब्रह्म का बीज: अक्षरों को ‘नाद’ या ‘ॐ’ (प्रणव) की अभिव्यक्ति माना गया। यह विचार अक्षर को केवल वर्णमाला का हिस्सा न मानकर, दैवीय सत्ता से जोड़ता है। प्राकृत भाषा ने अक्षरों को सहजता प्रदान कर उन्हें जनसामान्य तक पहुँचाया, जिससे विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति लोक-सुलभ हुई।
शब्द – जब अक्षर एक निश्चित अर्थ के साथ संयुक्त होते हैं, तो शब्द का निर्माण होता है। शब्द ही विचार और जगत के बीच सेतु है। आचार्य भर्तृहरि ने अपने ‘वाक्यपदीय’ में स्फोट सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार वास्तविक शब्द (स्फोट) एक अखंड, नित्य और अर्थ-वाहक इकाई है। शब्द-ब्रह्म को भर्तृहरि ने अंतिम सत्य माना। आचार्य मम्मट ने अपने ‘काव्यप्रकाश’ में शब्द की तीन शक्तियों का वर्गीकरण किया:
- सीधा और वाच्य अर्थ (जैसे ‘घोड़ा’ कहने पर पशु का बोध)।
- व्यंजना (ध्वन्यार्थ): रस की प्रतीति कराना।
- व्यंग्यार्थ (रस का वहन): अर्थ-संप्रेषण से अधिक रस की अनुभूति कराना।
वाक्य – रसात्मकता की कसौटी और काव्य की आत्मा शब्दों का सार्थक, आकांक्षापूर्ण और सन्निधियुक्त समूह वाक्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने ‘साहित्यदर्पण’ में कहा: “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्।” वह वाक्य जो केवल सूचना देता है, वह व्याकरणिक वाक्य तो है, पर काव्य नहीं। काव्य वाक्य वह है जो स्थायी भाव को विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के माध्यम से अलौकिक आनंद प्रदान करे।
ग्रंथ – ग्रंथ अक्षर, शब्द और रसात्मक वाक्यों का वह सुनिश्चित संयोजन है जो किसी उद्देश्य, दर्शन या ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी रूप प्रदान करता है। सूत्र ‘वानोच्छेदि जगत सर्वम्’ (संपूर्ण जगत वाणी में समाहित है) का चरम रूप ग्रंथ है। ग्रंथ ही वह माध्यम है जिसके द्वारा वेद, उपनिषद, दर्शन और कला का ज्ञान, जिसे अक्षर-मंत्र और रसात्मक वाक्य में पिरोया गया, काल की सीमाओं को पार कर जाता है। भारतीय साहित्यशास्त्र ने अक्षर को आध्यात्मिक आधार, शब्द को दार्शनिक शक्ति, वाक्य को कलात्मक प्राण (रस) और ग्रंथ को सभ्यता का मूर्त रूप प्रदान किया।
पतंजलि से लेकर विश्वनाथ तक, समस्त चिंतन इस बात पर केंद्रित रहा कि भाषा की इकाई, चाहे प्राकृत की सहजता में हो या संस्कृत की शुद्धता में, उसका अंतिम लक्ष्य परम-अर्थ और परम-आनंद की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि भारतीय आचार्यों ने अक्षर को अविनाशी मंत्र घोषित किया, जिससे शब्द, रसात्मक वाक्य और अंततः ग्रंथ के रूप में मानव चेतना का उच्चतम उत्कर्ष संभव हुआ। अक्षर, शब्द और वाक्य की त्रयी ही ग्रंथ रूप में भारतीय ज्ञान, कला और दर्शन का अविनाशी आधार है।