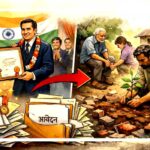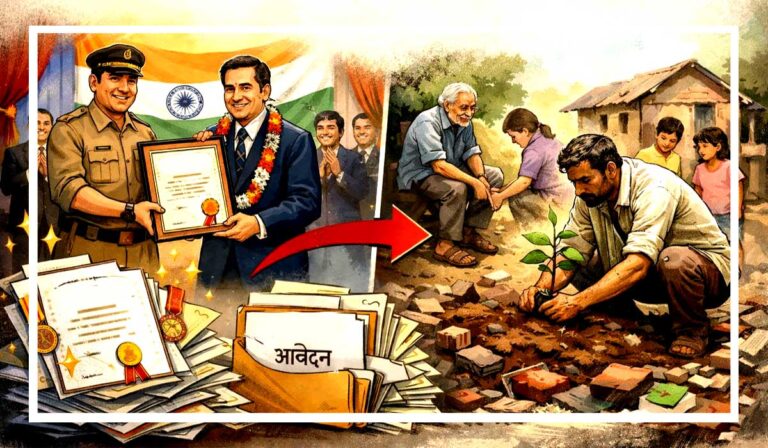देहरादून | हर वर्ष भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं से जूझने वाला उत्तराखंड अब आपदा प्रबंधन में तकनीकी क्रांति की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। दिल्ली में हाल ही में आयोजित “स्पेस मीट” (Space Meet) में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से हिमालयी राज्यों के लिए अलग सैटेलाइट समूह (Satellite Constellation) स्थापित करने की मांग रखी है। राज्य के आईटी सचिव नितेश झा ने इस बैठक में प्रदेश की ओर से प्रस्तुति देते हुए कहा कि —
“हिमालयी भू-भाग की जटिल भौगोलिक संरचना को देखते हुए मौजूदा सैटेलाइट डाटा पर्याप्त नहीं है। आपदाओं से पूर्व चेतावनी देने और वास्तविक समय में राहत कार्यों की निगरानी के लिए एक विशेष सैटेलाइट समूह की आवश्यकता है, जो केवल हिमालयी राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य करे।”
आपदा से पहले: उन्नत सैटेलाइट तकनीक से मिलेगी पूर्व चेतावनी
राज्य सरकार का कहना है कि अलग सैटेलाइट समूह से 50 सेंटीमीटर से कम की स्पष्टता वाले अत्यधिक उच्च-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट चित्र प्राप्त होंगे। इन चित्रों का उपयोग न केवल पहाड़ी क्षेत्रों की भू-आकृति (Topography) और ढलानों की स्थिति समझने में होगा, बल्कि संभावित भूस्खलन और बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान पहले से की जा सकेगी। इसके साथ ही राज्य ने मांग रखी है कि इस सैटेलाइट समूह में हाई-रिजॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) और LiDAR तकनीक (Light Detection and Ranging) को भी जोड़ा जाए। इन तकनीकों से ऊंचाई, स्थलाकृति और मिट्टी की नमी जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपदा की संभावना का वैज्ञानिक पूर्वानुमान संभव हो सकेगा। आईटी सचिव झा ने बताया कि —
“अगर हमें कुछ घंटे या दिन पहले ही सटीक डेटा मिल जाए, तो भूस्खलन, ग्लेशियर फटने या बादल फटने जैसी घटनाओं से भारी जनहानि को रोका जा सकता है। हमारा उद्देश्य पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है।”
हिमालयी राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए सटीक मॉडल
उत्तराखंड ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि सैटेलाइट समूह केवल मौसम, जलस्तर, हिमपात और वर्षा के पैटर्न की निगरानी तक सीमित न रहे, बल्कि इससे क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) पर भी सतत निगरानी रखी जाए। इसके लिए राज्य ने एक समर्पित ‘क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी’ (Climate Observatory) स्थापित करने का सुझाव दिया है, जो लगातार तापमान, आर्द्रता, बर्फ पिघलने की दर और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों पर नजर रख सके। उत्तराखंड का मानना है कि हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलता और भौगोलिक असमानता को देखते हुए, देश के सामान्य सैटेलाइट डेटा से यहां के खतरों की सटीक भविष्यवाणी कर पाना कठिन है।
Government Advertisement...
“अलग सैटेलाइट समूह” से राज्य-विशिष्ट मॉडल तैयार करना संभव होगा, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने में मदद करेगा। उत्तराखंड ने यह भी कहा कि आपदा के दौरान और बाद में संचार व्यवस्था सबसे पहले प्रभावित होती है। इसलिए राज्य ने मांग की है कि सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए, ताकि राहत और बचाव कार्यों में समन्वय बना रहे। सचिव झा ने बताया कि धराली, रैणी और जोशीमठ जैसी आपदाओं के दौरान जब ज़मीनी नेटवर्क ठप हो गया था, तब सैटेलाइट आधारित संचार तंत्र की अनुपस्थिति ने राहत कार्यों में बड़ी बाधा डाली। उन्होंने कहा —
“अगर हमारे पास सैटेलाइट आधारित रियल-टाइम संचार और इमेजिंग सिस्टम होता, तो राहत दल तुरंत संवेदनशील इलाकों तक पहुंच सकते थे।”
धराली आपदा से मिली सीख: बादलों के पार देखने वाली तकनीक जरूरी
धराली आपदा के दौरान घने बादलों के कारण सैटेलाइट तस्वीरें अस्पष्ट हो गई थीं। इस अनुभव से सबक लेते हुए राज्य ने केंद्र से “सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR)” जैसी उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने की मांग की है। SAR तकनीक बादलों और अंधेरे मौसम में भी स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम होती है। इससे आपदा के बाद इलाके की स्थिति, नदी अवरोध, अस्थायी झीलों और संभावित भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान की जा सकेगी। राज्य का कहना है कि इस तकनीक को अपनाने से मॉनसून सीजन में भी सटीक निगरानी संभव होगी, जिससे जीवन और संपत्ति की हानि को न्यूनतम किया जा सकेगा।
उत्तराखंड का यह प्रस्ताव केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र — हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों — के लिए भी एक दीर्घकालिक समाधान बन सकता है। यदि केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेती है, तो यह भारत के आपदा प्रबंधन तंत्र में ऐतिहासिक सुधार साबित होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि यह सैटेलाइट नेटवर्क न केवल पूर्व चेतावनी और राहत कार्यों को सशक्त बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, वनों की निगरानी, जलस्रोत प्रबंधन और पर्यटन योजनाओं में भी उपयोगी साबित होगा।