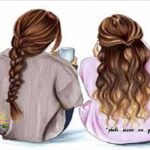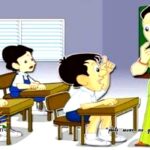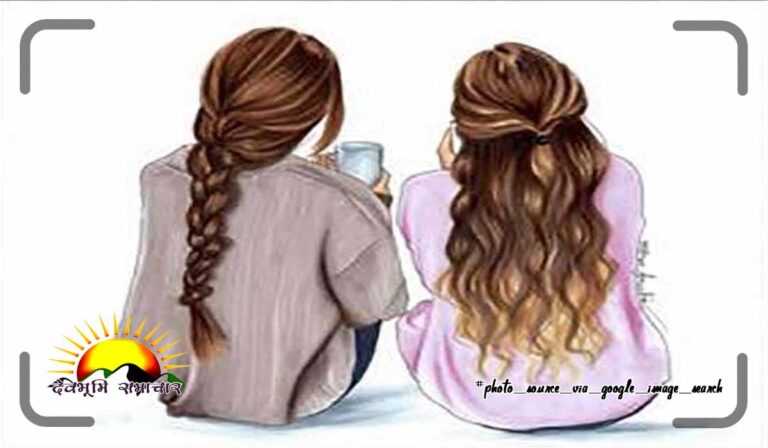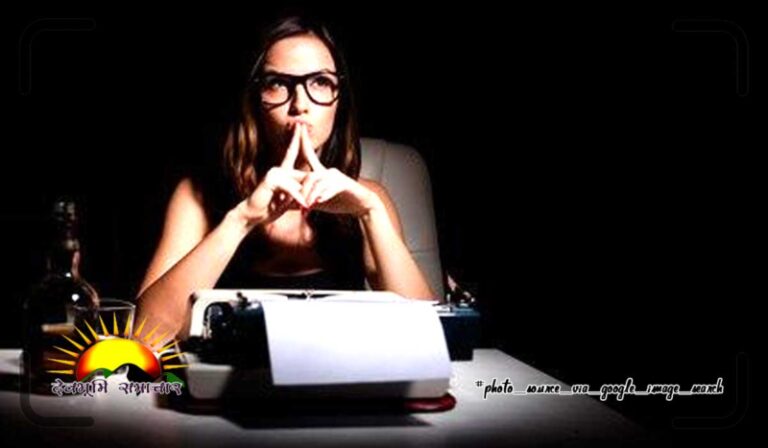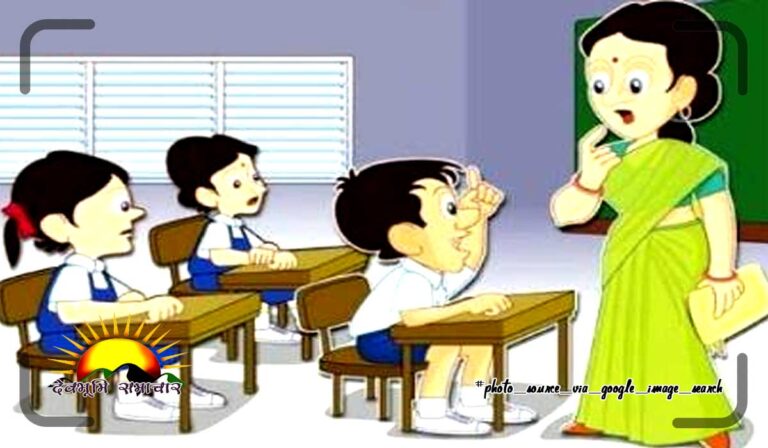– डॉ. प्रियंका सौरभ
 संविधान ने समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को स्थापित किया, परंतु भारतीय समाज में जाति चेतना अभी भी गहराई से विद्यमान है। शिक्षित और शहरी वर्गों में यह चेतना प्रत्यक्ष भेदभाव के बजाय सूक्ष्म रूपों में प्रकट होती है — जैसे रोजगार, विवाह और सामाजिक नेटवर्क में। आर्थिक प्रगति और आधुनिकता ने जाति को कमजोर किया है, पर समाप्त नहीं किया। व्यावसायिक क्षेत्रों में जातीय सामाजिक पूँजी अब भी अवसरों और संपर्कों को प्रभावित करती है। जब तक मानसिकता और व्यवहार में समानता स्थापित नहीं होती, तब तक संवैधानिक समानता का आदर्श अधूरा रहेगा। भारतीय समाज की संरचना में जाति एक ऐसी संस्था रही है जिसने व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन को प्रभावित किया है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता, नैतिकता और कर्म पर आधारित हो, न कि जन्मजात सामाजिक वर्ग पर। इसी उद्देश्य से संविधान में समानता का अधिकार, अवसरों की समानता, और अस्पृश्यता के उन्मूलन जैसी कई सुरक्षा धाराएँ जोड़ी गईं। किंतु सात दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी यह स्वीकार करना होगा कि जाति की चेतना केवल गाँवों तक सीमित नहीं रही; उसने शिक्षित, शहरी और व्यावसायिक तबकों में भी अपने बदले हुए स्वरूप में अस्तित्व बनाए रखा है।
संविधान ने समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को स्थापित किया, परंतु भारतीय समाज में जाति चेतना अभी भी गहराई से विद्यमान है। शिक्षित और शहरी वर्गों में यह चेतना प्रत्यक्ष भेदभाव के बजाय सूक्ष्म रूपों में प्रकट होती है — जैसे रोजगार, विवाह और सामाजिक नेटवर्क में। आर्थिक प्रगति और आधुनिकता ने जाति को कमजोर किया है, पर समाप्त नहीं किया। व्यावसायिक क्षेत्रों में जातीय सामाजिक पूँजी अब भी अवसरों और संपर्कों को प्रभावित करती है। जब तक मानसिकता और व्यवहार में समानता स्थापित नहीं होती, तब तक संवैधानिक समानता का आदर्श अधूरा रहेगा। भारतीय समाज की संरचना में जाति एक ऐसी संस्था रही है जिसने व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन को प्रभावित किया है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता, नैतिकता और कर्म पर आधारित हो, न कि जन्मजात सामाजिक वर्ग पर। इसी उद्देश्य से संविधान में समानता का अधिकार, अवसरों की समानता, और अस्पृश्यता के उन्मूलन जैसी कई सुरक्षा धाराएँ जोड़ी गईं। किंतु सात दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी यह स्वीकार करना होगा कि जाति की चेतना केवल गाँवों तक सीमित नहीं रही; उसने शिक्षित, शहरी और व्यावसायिक तबकों में भी अपने बदले हुए स्वरूप में अस्तित्व बनाए रखा है।
संविधान ने अनुच्छेद 14 से 17 के माध्यम से स्पष्ट रूप से सभी नागरिकों को समानता और सम्मान का अधिकार दिया। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसे केवल विधिक समानता का नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता का माध्यम बताया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि सामाजिक असमानता बनी रही तो राजनीतिक समानता टिक नहीं सकेगी। यह चेतावनी आज भी प्रासंगिक प्रतीत होती है, क्योंकि कानून की शक्ति के बावजूद समाज की मानसिकता में गहराई से जमी जाति-आधारित सोच पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। शिक्षा को सामाजिक चेतना का वाहक माना जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिक्षित वर्ग में भी जातीय पूर्वाग्रह सूक्ष्म और परिष्कृत रूपों में जीवित हैं। विश्वविद्यालयों और पेशेवर संस्थानों में प्रवेश के दौरान, सहकर्मी संबंधों में या सामाजिक नेटवर्किंग में अक्सर जाति एक अनकही पहचान के रूप में उपस्थित रहती है। ‘मेरिट’ की चर्चा करते हुए कई बार लोग आरक्षण नीति को लेकर पूर्वाग्रह रखते हैं और यह मान बैठते हैं कि आरक्षित वर्गों के लोग स्वाभाविक रूप से कम योग्य हैं। यह धारणा आधुनिक भारत के शिक्षित तबके में भी समानता के सिद्धांत को चुनौती देती है।
शहरीकरण और औद्योगीकरण को जातीय सीमाओं को तोड़ने वाला माना गया था। परंतु व्यवहार में देखा जाए तो शहरों में भी जातीय चेतना नई संरचनाओं में पुनर्जीवित हुई है। उदाहरण के लिए, महानगरों में भी अधिकांश लोग अपने ही जाति-समूहों में विवाह करते हैं। ‘मैट्रिमोनी वेबसाइट्स’ पर जाति और उपजाति आज भी प्रमुख फ़िल्टर के रूप में मौजूद हैं। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक प्रगति और आधुनिकता ने बाहरी व्यवहार को तो बदला है, परंतु सामाजिक मनोविज्ञान अब भी जाति के घेरे से मुक्त नहीं हो सका है। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी जाति की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। पारंपरिक रूप से व्यापार और व्यवसाय कुछ खास जातियों के वर्चस्व में रहे हैं, और आधुनिक कॉर्पोरेट ढाँचे में भी यह प्रवृत्ति अप्रत्यक्ष रूप से जारी है। नेटवर्किंग, निवेश और अवसरों तक पहुँच में जातीय सामाजिक पूँजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरणस्वरूप, किसी व्यापारिक समुदाय के सदस्य एक-दूसरे को व्यवसायिक सहयोग देना अधिक सहज समझते हैं। इसी तरह नौकरियों में भर्ती या पदोन्नति के दौरान ‘सांस्कृतिक मेल’ या ‘नेटवर्क फिट’ जैसे अस्पष्ट मानदंडों के तहत कई बार सामाजिक पूर्वाग्रह सक्रिय रहते हैं।
राजनीतिक रूप से भी जाति चेतना ने आधुनिक लोकतंत्र में नई ऊर्जा प्राप्त की है। शहरी मध्यम वर्ग स्वयं को अक्सर जाति से ऊपर बताता है, लेकिन चुनावों के दौरान वही वर्ग जातिगत पहचान के आधार पर अपनी निष्ठा तय करता दिखाई देता है। जातीय संगठन, छात्र संघ और पेशेवर एसोसिएशन अब अपनी जातिगत पहचान को अधिकारों की माँग से जोड़ रहे हैं। इस तरह जाति अब केवल सामाजिक संस्था नहीं रही, बल्कि यह ‘राजनीतिक संसाधन’ और ‘सामाजिक पूँजी’ का रूप ले चुकी है।भारत में शहरी क्षेत्रों में जाति का यह रूप प्रकट भेदभाव की अपेक्षा सांकेतिक भेदभाव के रूप में उभरता है। किसी को उसकी जाति के कारण सीधे अपमानित करना अब कानूनन अपराध है, परंतु सूक्ष्म रूपों में यह मानसिकता सामाजिक जीवन में व्याप्त रहती है। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी के सामाजिक पृष्ठभूमि का उपहास करना, आरक्षण को लेकर तंज कसना, या सहकर्मी के साथ सामाजिक दूरी बनाकर रखना — ये सब जाति-आधारित पूर्वाग्रह के ही रूप हैं।
डिजिटल युग में जातीय चेतना ने एक नया माध्यम प्राप्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जातीय समूहों के पेज, संगठन और समुदाय अपने गौरव और इतिहास का प्रचार करते हैं। यह सांस्कृतिक आत्मसम्मान का प्रतीक हो सकता है, लेकिन कई बार यह प्रतिस्पर्धात्मक जातीयता में बदल जाता है, जिससे समाज में नये विभाजन पैदा होते हैं। ‘हम’ बनाम ‘वे’ की मानसिकता अब वर्चुअल दुनिया में भी कायम है।आर्थिक उदारीकरण के बाद माना गया था कि वैश्विक बाजार और निजी क्षेत्र में योग्यता ही सर्वोपरि होगी। परंतु 1990 के दशक से लेकर आज तक के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी दलित और पिछड़े वर्गों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के कारण यह असमानता और बढ़ी है। परिणामस्वरूप, आधुनिकता और बाजारवाद ने समान अवसरों का भ्रम तो दिया, परंतु जातीय असमानता की वास्तविकता को समाप्त नहीं कर पाया।
शहरी मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा जाति को औपचारिक रूप से अस्वीकार करता है, परंतु अनौपचारिक जीवन में यह वर्ग जाति-संबंधी पहचानों का उपयोग करता है। यह विरोधाभास आधुनिक भारत की सामाजिक जटिलता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कार्यालय में स्वयं को उदारवादी बताता है, लेकिन विवाह के लिए अपने बच्चों के लिए जाति आधारित विकल्प ही स्वीकार करता है। इस दोहरे व्यवहार से स्पष्ट होता है कि जाति का सामाजिक प्रभाव अब भी जीवन के सबसे निजी निर्णयों तक पहुँचा हुआ है। जातीय चेतना की निरंतरता का एक कारण यह भी है कि समाज में जाति अब केवल उत्पीड़न का प्रतीक नहीं, बल्कि पहचान और समुदाय के सहारे के रूप में भी देखी जाने लगी है। विशेषकर आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति के बाद वंचित समूहों ने जाति को अपने अधिकारों की रक्षा का माध्यम बनाया है। इससे जाति का एक ‘सकारात्मक विमर्श’ भी उभरा है, जो आत्मसम्मान और प्रतिनिधित्व की बात करता है। किंतु इस प्रक्रिया में जाति की सीमाएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं, बल्कि उनका रूपांतर हो गया।
सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय शहरी समाज में अब जाति एक “रिसोर्स नेटवर्क” बन चुकी है। यह पारंपरिक बंधन से निकलकर आधुनिक संपर्क माध्यम बन गई है। नौकरी, व्यवसाय या राजनीति में यह अब भी विश्वास, सहयोग और संसाधनों के वितरण का आधार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिकता ने जाति को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे नए रूप में ढाल दिया। संवैधानिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते समय यह भी समझना आवश्यक है कि कानून केवल ढाँचा प्रदान कर सकता है, लेकिन सामाजिक चेतना का परिवर्तन धीरे-धीरे ही होता है। शिक्षा और आर्थिक प्रगति ने जातीय असमानता को चुनौती दी है, परंतु सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन की गति धीमी है। जब तक सामाजिक सम्मान, अवसर और पहचान का आधार व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता न होकर समूहगत पहचान रहेगी, तब तक जातीय चेतना बनी रहेगी।
समाजशास्त्री आंद्रे बेतिए, एम.एन. श्रीनिवास और गोपीनाथ मोहंती जैसे विचारकों ने बार-बार यह बताया कि भारत में शहरीकरण का अर्थ पारंपरिक ढाँचों का पूर्ण विघटन नहीं, बल्कि उनका पुनर्संयोजन है। यानी, गाँव की जाति व्यवस्था का बाहरी रूप भले टूटे, पर उसकी मानसिकता शहर में नए रूप में पुनः निर्मित हो जाती है। यही कारण है कि आईटी सेक्टर, मीडिया, शिक्षा, और चिकित्सा जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी जाति से जुड़ी असमानताएँ सूक्ष्म रूपों में विद्यमान हैं। जातीय चेतना की यह निरंतरता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इसलिए कि यह समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को सीमित करती है, और अवसर इसलिए कि इस चेतना को सामाजिक न्याय के व्यापक विमर्श में बदला जा सकता है। यदि जाति का प्रयोग उत्पीड़न के बजाय प्रतिनिधित्व और सहयोग के साधन के रूप में किया जाए, तो यह सामाजिक सामंजस्य को बल दे सकती है।
आगे का मार्ग शिक्षा, संवेदनशीलता और नीति-निर्माण के संयोजन में निहित है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सामाजिक विविधता और समानता पर आधारित मूल्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यस्थलों पर विविधता को बढ़ावा देने के लिए एथिक्स कोड, समान अवसर आयोग और असमानता पर स्वतंत्र ऑडिट प्रणाली जैसी व्यवस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं। मीडिया और जनसंचार माध्यमों को भी जातीय रूढ़ियों को तोड़ने और समानता के आदर्श को प्रचारित करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। भारत का संविधान केवल विधि का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का घोषणापत्र है। इसकी भावना यह कहती है कि व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म से आँका जाए, न कि उसके जन्म से। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षित और कार्यरत वर्ग — जो समाज में अनुकरणीय भूमिका निभाता है — वह स्वयं इस परिवर्तन का नेतृत्व करे। जब तक सामाजिक सम्मान, अवसर और व्यवहार में जाति की भूमिका समाप्त नहीं होगी, तब तक समानता का सपना अधूरा रहेगा।
अंततः कहा जा सकता है कि भारत का समाज परिवर्तनशील है, किंतु जाति चेतना उसकी सबसे गहरी जड़ है। संविधान ने हमें दिशा दी, लेकिन सामाजिक यथार्थ ने अब तक उस दिशा में पूर्ण यात्रा नहीं की। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार ने जाति को कमजोर अवश्य किया है, परंतु उसका प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ। आधुनिक भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह कानून और व्यवहार, दोनों में समानता का आदर्श साकार करे। तभी हम उस भारत की कल्पना को साकार कर पाएँगे जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं, बल्कि उसकी मानवीयता होगी।
— प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंस
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार
उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)