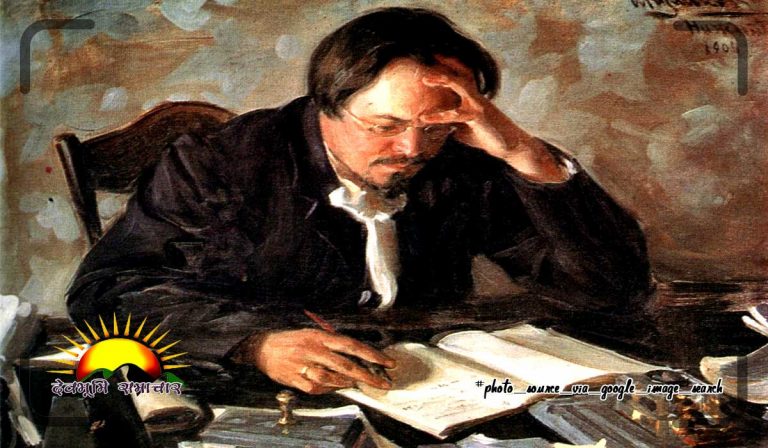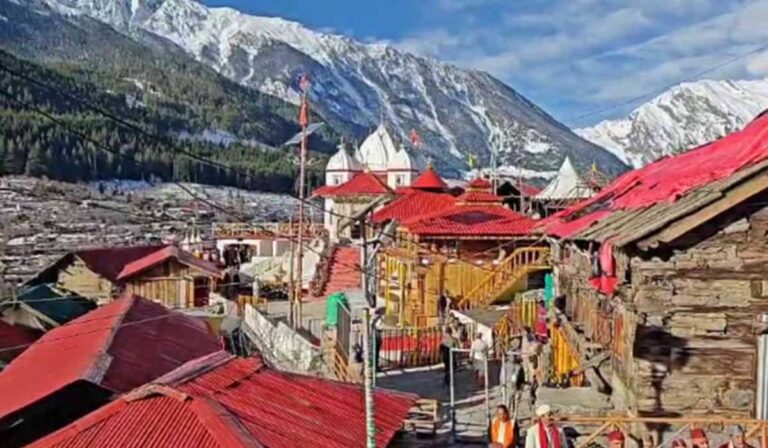डॉ॰ सत्यवान सौरभ
 इंस्टाग्राम ने 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को आपत्तिजनक कंटेंट से दूर रखने के लिए PG-13 आधारित फ़िल्टर प्रणाली लागू की है। इससे नाबालिग यूज़र्स हिंसक, यौन या मानसिक रूप से हानिकारक सामग्री नहीं देख पाएंगे। माता-पिता अब “सीमित कंटेंट सेटिंग्स” से बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे। यह कदम सोशल मीडिया पर किशोरों की सुरक्षा और मानसिक संतुलन की दिशा में एक बड़ी पहल है। यदि इसे गंभीरता से लागू किया गया, तो यह स्वस्थ और जिम्मेदार डिजिटल समाज के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। डिजिटल युग में सोशल मीडिया आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बच्चा हो या बड़ा, सबकी दिनचर्या का एक अहम समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बीतता है। लेकिन जैसे-जैसे इस आभासी दुनिया की चमक बढ़ी है, वैसे-वैसे इससे जुड़े खतरे भी गहराते गए हैं। सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं किशोर, जिनकी सोच, मनोवृत्ति और व्यवहार अभी विकसित हो ही रहे हैं।
इंस्टाग्राम ने 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को आपत्तिजनक कंटेंट से दूर रखने के लिए PG-13 आधारित फ़िल्टर प्रणाली लागू की है। इससे नाबालिग यूज़र्स हिंसक, यौन या मानसिक रूप से हानिकारक सामग्री नहीं देख पाएंगे। माता-पिता अब “सीमित कंटेंट सेटिंग्स” से बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे। यह कदम सोशल मीडिया पर किशोरों की सुरक्षा और मानसिक संतुलन की दिशा में एक बड़ी पहल है। यदि इसे गंभीरता से लागू किया गया, तो यह स्वस्थ और जिम्मेदार डिजिटल समाज के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। डिजिटल युग में सोशल मीडिया आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बच्चा हो या बड़ा, सबकी दिनचर्या का एक अहम समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बीतता है। लेकिन जैसे-जैसे इस आभासी दुनिया की चमक बढ़ी है, वैसे-वैसे इससे जुड़े खतरे भी गहराते गए हैं। सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं किशोर, जिनकी सोच, मनोवृत्ति और व्यवहार अभी विकसित हो ही रहे हैं।
सोशल मीडिया की चकाचौंध में खोए किशोरों के लिए यह प्लेटफॉर्म कभी-कभी सीख का माध्यम तो बनता है, परंतु कई बार यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक असंतुलन का कारण भी बन जाता है। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक या अनुचित कंटेंट नहीं देख पाएंगे। यह फैसला केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति का मन सबसे संवेदनशील होता है। इस उम्र में जो कुछ देखा, सुना और महसूस किया जाता है, वही आने वाले जीवन की दिशा तय करता है। सोशल मीडिया पर हिंसक, यौन संकेतक या अवसादपूर्ण सामग्री तक आसान पहुँच बच्चों को अनजाने में ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ से लौटना कठिन हो जाता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति, अवसाद, असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी जैसी मानसिक समस्याएँ सोशल मीडिया की असंयमित दुनिया से गहराई तक जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मेटा का यह निर्णय निश्चय ही एक जिम्मेदार पहल है।
मेटा ने यह नीति ऐसे समय में बनाई है जब दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस चल रही है। कई देशों की संसदों और अदालतों में सोशल मीडिया कंपनियों से यह पूछा गया कि वे नाबालिगों की मानसिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही हैं। इंस्टाग्राम पर किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कंपनी पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस से लेकर ब्रिटिश संसदीय समितियों तक में यह मुद्दा गूंज चुका है। मेटा के पूर्व कर्मचारियों ने भी यह खुलासा किया था कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिद्म किशोरों को अधिक समय तक प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए जानबूझकर ऐसे कंटेंट सुझाता है जो मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है। आलोचनाओं के बाद कंपनी ने ‘पैरेंटल सुपरविजन टूल्स’ शुरू किए थे, लेकिन वे सीमित थे। अब कंपनी ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए “PG-13 आधारित कंटेंट फ़िल्टरिंग सिस्टम” लागू करने का निर्णय लिया है।
इस नई व्यवस्था के तहत माता-पिता को यह अधिकार होगा कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकें। 18 वर्ष से कम आयु के यूजर्स को इंस्टाग्राम पर वह सामग्री स्वतः ही नहीं दिखाई देगी जो हिंसक, यौन या आत्मघाती प्रवृत्ति वाली हो। यह प्रणाली फ़िल्टर के माध्यम से काम करेगी जो हॉलीवुड फिल्मों की PG-13 रेटिंग प्रणाली की तरह होगी। जैसे किसी फिल्म को यह रेटिंग तब दी जाती है जब वह 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, वैसे ही अब इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट की उपयुक्तता उसी मानक से तय की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह फीचर पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लागू होगा और वर्ष के अंत तक भारत सहित दुनिया भर में लागू कर दिया जाएगा।
यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सोशल मीडिया यूजर्स के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में है। लाखों किशोर रोजाना इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे सेल्फी पोस्ट करने, रील्स बनाने और लाइक्स पाने की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि वास्तविक जीवन की संवेदनाएं और प्राथमिकताएं पीछे छूटती जा रही हैं। किशोरों का आत्ममूल्य अब इस बात से तय होने लगा है कि उन्हें कितने फॉलोअर्स मिले, कितने लोगों ने उनकी पोस्ट को पसंद किया। यह सामाजिक स्वीकृति का नया और खतरनाक रूप है। जब किसी पोस्ट पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो किशोर आत्मग्लानि और अवसाद में डूबने लगते हैं। कई बार इसी निराशा में वे आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। ऐसे में अगर इंस्टाग्राम किशोरों को आपत्तिजनक सामग्री से दूर रख सके तो यह उनके मानसिक संतुलन और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।
माता-पिता भी इस कदम से राहत महसूस करेंगे। अब उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि उनका बच्चा गलती से किसी गलत दिशा में जा रहा है या अश्लील सामग्री के प्रभाव में आ रहा है। “सीमित कंटेंट सेटिंग्स” के ज़रिए वे यह तय कर पाएंगे कि उनके बच्चे को क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं। इससे पारिवारिक संवाद भी बेहतर होगा क्योंकि अभिभावक अब निगरानी के साथ-साथ मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकेंगे। बच्चों को भी यह एहसास होगा कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने का प्लेटफॉर्म है। फिर भी यह नीति तभी सफल होगी जब तकनीकी सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी बढ़े। केवल फिल्टर लगाने से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। बच्चे हमेशा तकनीक से एक कदम आगे रहते हैं। वे प्रतिबंधों को पार करने के तरीके खोज लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्कूलों, परिवारों और समाज में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। बच्चों को यह समझाया जाए कि क्या सही है, क्या गलत है और क्यों कुछ चीज़ें सीमित की जा रही हैं। जब तक उन्हें कारणों की समझ नहीं होगी, वे प्रतिबंधों को नियंत्रण नहीं बल्कि विरोध के रूप में देखेंगे।
यह भी विचारणीय है कि “आपत्तिजनक सामग्री” की परिभाषा हर समाज और संस्कृति में अलग-अलग हो सकती है। जो एक देश में अनुचित माना जाता है, वह दूसरे में सामान्य हो सकता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर लागू होने वाले ऐसे नियमों के लिए सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। मेटा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके एल्गोरिद्म स्थानीय भाषाओं और समाज की संवेदनशीलता को समझ सकें। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों की प्राथमिकता प्रायः मुनाफा होती है, न कि नैतिकता। अधिक यूजर्स का मतलब अधिक विज्ञापन और अधिक राजस्व। ऐसे में किशोरों को प्लेटफॉर्म से दूर रखना या उनके कंटेंट को सीमित करना कंपनी के आर्थिक हितों के विपरीत जा सकता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि मेटा इस नई नीति को कितनी गंभीरता से लागू करता है। यदि यह केवल दिखावटी कदम साबित हुआ तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
सोशल मीडिया के नियमन की यह वैश्विक पहल सरकारों के लिए भी एक संकेत है। डिजिटल दुनिया इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि अब केवल नैतिक अपीलों से काम नहीं चलेगा। जैसे फिल्मों, विज्ञापनों और टीवी कार्यक्रमों पर सेंसरशिप की एक व्यवस्था होती है, वैसे ही सोशल मीडिया के लिए भी संतुलित और स्वतंत्र निगरानी संस्थान आवश्यक हैं। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनियां केवल नीतियां घोषित न करें बल्कि उनके पालन के लिए पारदर्शी तंत्र भी बनाएं। अभिभावकों को भी सशक्त किया जाए कि वे अपने बच्चों की डिजिटल आदतों पर नज़र रख सकें। किशोरों को यह समझाने की ज़रूरत है कि इंस्टाग्राम पर लाइक्स या फॉलोअर्स से उनकी असली पहचान तय नहीं होती। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक सहयोग ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं। डिजिटल दुनिया असली दुनिया का विकल्प नहीं हो सकती। अगर बच्चे यह समझ जाएँ कि सोशल मीडिया एक साधन है, साध्य नहीं, तो उसकी सकारात्मक क्षमता अपार है।
मेटा का यह निर्णय केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि एक मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में किशोर आत्महत्या, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण के शिकार हो रहे हैं, तब ऐसी पहलें उम्मीद की किरण बनती हैं। लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया कंपनियाँ पारदर्शिता बरतें। माता-पिता को नियमित रिपोर्ट्स मिलें, बच्चे स्वयं अपने डिजिटल व्यवहार का मूल्यांकन करें और शिक्षण संस्थान इस विषय को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। कई अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि सोशल मीडिया की अधिकता से किशोरों में चिंता, नींद की कमी और आत्मसंतुष्टि में गिरावट आती है। लगातार दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति उन्हें हीनभावना की ओर धकेल देती है। “परफेक्ट बॉडी”, “ग्लैमरस लाइफस्टाइल” और “फिल्टर की दुनिया” में वे असलियत से कटते चले जाते हैं। मेटा यदि अपने नए सिस्टम के ज़रिए इन खतरों को कम कर सके तो यह समाज के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
हालाँकि, इसे केवल किशोरों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वयस्कों के लिए भी सोशल मीडिया पर नियंत्रण आवश्यक है। फेक न्यूज़, घृणास्पद भाषण और गलत सूचनाएँ अब लोकतंत्र के लिए चुनौती बन चुकी हैं। इसलिए इस दिशा में मेटा की पहल अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए भी मिसाल बन सकती है। अंततः कहा जा सकता है कि यह निर्णय किशोरों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक विकास के लिए अत्यंत सराहनीय कदम है। तकनीक तभी सार्थक होती है जब वह मानवता की भलाई के लिए काम करे। मेटा का यह कदम इसी भावना का विस्तार है। आने वाले समय में यदि यह नीति पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से लागू होती है, तो यह न केवल किशोरों बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक स्वस्थ डिजिटल संस्कृति की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित होगी।
— डॉ॰ सत्यवान सौरभ
कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पैनलिस्ट, 333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा