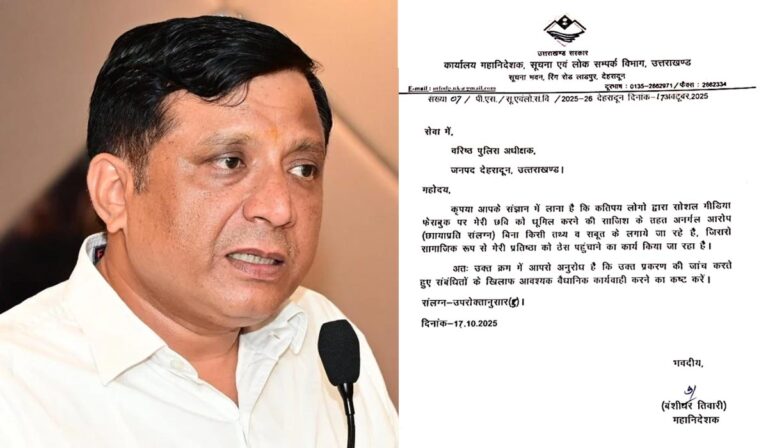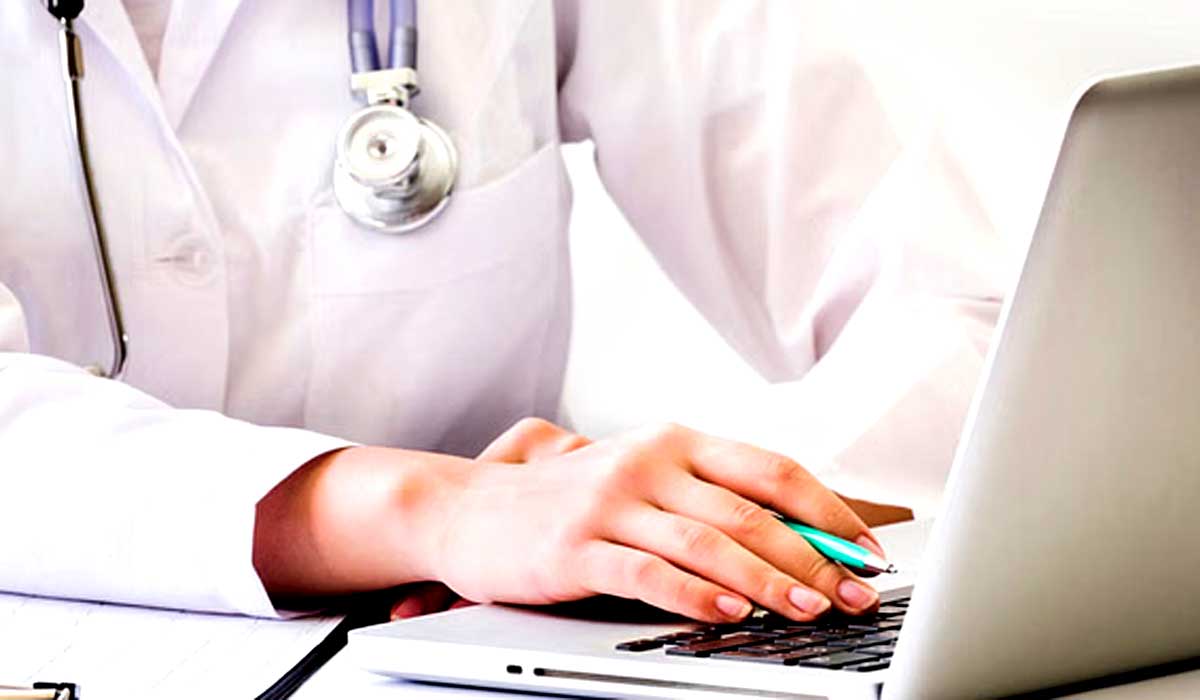
ऋषिकेश। उत्तराखंड में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन (Stunting) तेजी से घट रहा है, लेकिन पौड़ी और चमोली ज़िले इस मामले में अपवाद साबित हो रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, जहाँ पूरे प्रदेश में स्थिति सुधरी है, वहीं इन दोनों पहाड़ी जिलों में बच्चों का कद छोटा होने की समस्या बढ़ रही है। एम्स ऋषिकेश के सामुदायिक चिकित्सा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. वर्तिका सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2005 में राज्य में पांच साल से कम उम्र के 44 प्रतिशत बच्चे ठिगनापन से प्रभावित थे। वर्ष 2021 तक यह आँकड़ा घटकर 27 प्रतिशत पर आ गया। यानी ठिगनापन में कमी की दर 7 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड इस समस्या को घटाने के मामले में 8वें स्थान पर है।
लेकिन चिंता की बात यह है कि जहाँ राज्य स्तर पर सुधार हुआ है, वहीं चमोली ज़िले में ठिगनापन में 0.4 प्रतिशत और पौड़ी ज़िले में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रवृत्ति गंभीर है और इसके कारणों को समझने के लिए अलग से शोध ज़रूरी है। एम्स ने इस दिशा में पहल करते हुए राज्य सरकार से सहयोग मांगा है। देशभर में तुलना करें तो सिक्किम और मध्यप्रदेश ने ठिगनापन घटाने में 7.7 प्रतिशत की दर से प्रगति की है। सिक्किम में अब 22.3 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 35 प्रतिशत बच्चे इस समस्या से ग्रस्त हैं। राजस्थान 7.2 प्रतिशत की दर से घटाव के साथ दूसरे स्थान पर है, जहाँ 31.8 प्रतिशत बच्चे ठिगनापन के शिकार हैं।
प्रो. वर्तिका ने बताया कि उत्तराखंड में इस दिशा में सुधार योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। विशेष रूप से “कुपोषित बच्चों को गोद लेने” की योजना, जिसे मंगेश घिल्डियाल ने रुद्रप्रयाग के डीएम रहते शुरू किया था, अहम साबित हुई है। इसके साथ ही आंचल अमृत योजना, बाल पलाश योजना, महालक्ष्मी किट योजना और मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना भी पोषण सुधार में बड़ी भूमिका निभा रही हैं।
✍ आपकी आवाज़, हमारी आवाज़… “देवभूमि समाचार”
बच्चों में ठिगनापन केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के शारीरिक और मानसिक विकास से जुड़ा बड़ा सवाल है। राज्य में योजनाओं से सुधार दिख रहा है, लेकिन पौड़ी और चमोली जैसे जिलों में हालात बिगड़ना कई सवाल खड़े करता है—
- क्या पहाड़ी इलाकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच अब भी कमजोर है?
- क्या पलायन, बेरोज़गारी और सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ बच्चों के कुपोषण को बढ़ा रही हैं?
- क्या स्थानीय खानपान और जीवनशैली में बदलाव भी ठिगनापन बढ़ने की वजह बन रहे हैं?
- सरकार को किस तरह की नई योजनाएँ या नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि सभी जिलों में समान रूप से सुधार हो सके?
आपकी नज़र में इस समस्या से निपटने के लिए कौन-से ठोस कदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? अपनी राय, सुझाव और अनुभव हमारे साथ साझा करें।