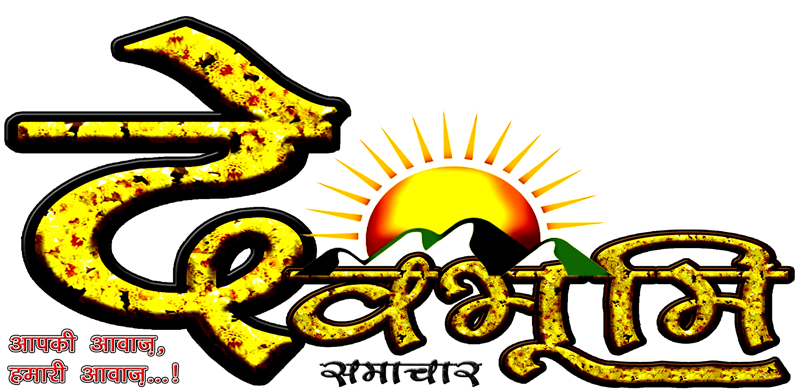जनतंत्र को “भ्रष्टतंत्र” में तब्दील करती पूंजीवादी सरकारें

अशोक शर्मा
पूँजीवादी सरकारें पहले उन संस्थानों पर अपना क़ब्ज़ा मज़बूत करती है, जो जनतांत्रिक परिवर्तन के कारण अस्तित्व में आये हैं और जिनसे जनतंत्र की दिनचर्या बनती है। ये संस्थान हैं- संसद, संविधान और क़ानून, मीडिया, न्यायपालिका, नौकरशाही, चुनाव और मताधिकार, न्यायिक बराबरी, नागरिक अधिकार आदि। दूसरी तरफ़ आम जनता भी अपनी आज़ादी और उन अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहती है, जिन्हें उसने क़ुर्बानी देकर हासिल किया होता है। कालांतर में प्रभुत्वशाली पूँजीवादी तबक़े मध्यवर्ग की मदद से इन्हीं संस्थानों को योजनाबद्ध तरीक़े से कमज़ोर करने में लग जाते हैं।
वे व्यवस्था के प्रति आम निराशा और वितृष्णा पैदा करने, अवाम के बीच राजनीति मात्र से नफ़रत का भाव पैदा करने, कल्याणकारी नीतियों को समाप्त करने और राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण में लग जाते हैं। जनतंत्र की सारवस्तु नष्ट कर दी जाती है। बस, एक खोखला ढाँचा बचा रह जाता है, जिस पर पूँजी के कारकुन तैनात रहते हैं। अंत में सिर्फ एक चीज़ रह जाती है-वोट, जिसे आप चाहे कांग्रेस को दें या भाजपा को, राजद को दें या जदयू को, नरेंद्र मोदी को दें या सोनिया को, मुलायम+मायावती को दें या लालू+नितीश को।
अवाम तो जनतंत्र को अपने हक़ में बदलना चाहते हैं, लेकिन वे उसे एक स्वाधीन, दासताहीन, सुरक्षित समाज और कल्याणकारी भविष्य के निर्माण के औज़ार में न बदल सकें, इसके लिए सरमायेदार तबक़ा विभाजनकारी हथकंडे अपनाता है। वह सांप्रदायिकीकरण, गुंडाराज, दुष्प्रचार, राजकीय आतंक, भ्रष्टाचार, अंध राष्ट्रवाद, सैन्यीकरण, युद्ध, तानाशाही, फ़ासीवाद वग़ैरह सारी जन-विरोधी चीज़ों का रास्ता खोल देता है। मोटे तौर पर पूँजीवाद का यही इतिहास रहा है। इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, जिसे आज़ाद हिंदुस्तान की जनता ने इन सड़सठ वर्षों में न देखा हो, और आज मुल्क के किसी न किसी हिस्से में हरदम न झेल रही हो। लगातार होने वाले जनसंहार, हर तरह का दमन, उत्पीड़न, शोषण, भूख, बीमारी और कुपोषण, बेरोज़गारी, विस्थापन, विषमता और अन्याय से “संसार के विशालतम जनतंत्र” का पूरा जिस्म दाग़दार है।
आज हिंदुस्तान में समाचार और प्रचार का तंत्र ही नहीं, पूरी ‘सार्वजनिक बुद्धि’ ही आपराधिक पूँजी के हाथ में है और यह अवाम को अराजनीतिक बनाने का मुख्य औज़ार है।समाचार पत्र और टेलीविज़न की अर्थव्यवस्था पर विज्ञापन के ज़रिये नियंत्रण और दूसरे, इन माध्यमों पर पूँजीपतियों का सीधा स्वामित्व और नियंत्रण। जिस तरह संपादकों, संवाददाताओं, कॉलम लेखकों, एंकरों, संयोजक जिन तरकीबों से वे पेशेवर बुद्धिजीवी वर्ग की मदद से ‘‘नये भारत’’ की तस्वीर बनाते हैं और ‘‘नया ज्ञान’’ हम तक पहुँचाते हैं, इस पर ग़ौर करने की ज़रूरत है।
हर तरफ़ से पूँजी का आक्रमण है। हताशा की हालत तो है। हताशा एक सच्चाई है।
ये लोग पाठक और दर्शक को निष्क्रिय, हताश और अराजनीतिक उपभोक्ता में बदलते हैं-उपभोक्ताओं की ऐसी भीड़ में, जिसकी सामान्य जनतांत्रिक चेतना मर चुकी हो, बल्कि जनतंत्र में तो जनता की राजनीतिक चेतना बढ़नी चाहिए, लेकिन भारतीय जनतंत्र में वह कम होती गयी और ज्यादातर लोग अराजनीतिक होते गये। जिसका जनतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर से विश्वास उठ चुका हो, जो खुद अपनी ताक़त में विश्वास खो चुकी हो, और जो यह मानने को तैयार हो कि अब या तो सुप्रीम कोर्ट या भगवान या कोई चमत्कारी पुरुष या फ़ौजी शासन या फ़ासीवाद ही इस देश को बचा सकता है। इस माहौल को बनाने में मीडिया का योगदान सबसे ज़्यादा है। मीडिया जनसंहार के दोषी एक विश्व प्रसिद्ध मानवद्रोही हत्यारे को विकास पुरुष, एक संदिग्ध एन.जी.ओ. ऑपरेटर को आम आदमी का उद्धारक, कुछ सस्ते ठगों को राष्ट्रीय महत्त्व के संत-राजनेताओं में बदलकर ‘विकल्प’ की तरह खड़े कर देता है। इस तरह देखें, तो विकल्प का निर्माण भी सत्ताधारियों के ही हाथ में है।
भारत को विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कहा जाता है, लेकिन भारत की जनता का उससे केवल वोट देने तक का या हद से हद अपने अधिकारों के लिए आंदोलन और संघर्ष करने तक का ही संबंध है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन वास्तव में सत्ता का केंद्रीकरण होता रहा है, जिससे नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में लोगों की कोई वास्तविक भूमिका और भागीदारी नहीं हो पाती है। उनके द्वारा चुने गये जन-प्रतिनिधि सत्ता में आने के बाद उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि उनके आंदोलनों और संघर्षों का दमन ही अधिक करते हैं। इससे पैदा होने वाली हताशा ही लोगों के अराजनीतिक होते जाने का कारण है
भारत की जनता इतनी अधिकारहीन पहले कभी न थी-ख़ासकर आदिवासी और मुसलमान जन, भूमिहीन लोग, और दलित जन का बहुलांश। निजीकरण, कांट्रैक्ट सिस्टम, छँटनी और दमनकारी कानूनसाजी के माध्यम से नये भारत के विधाताओं ने सबसे निबट लिया है। इन परिस्थितियों में सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ भी राज्य और जनपद के स्तर पर दलालों की एक फ़ौज खड़ी करना ही है। मूल रूप से तो हम एक दमनकारी पुलिस राज और सैन्यीकृत राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जनतांत्रिक संस्थाओं पर जनतंत्र के शत्रुओं का क़ब्ज़ा होता गया है। ये वे शत्रु हैं, जो जनतंत्र को ढाने के लिए जनतंत्र की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय मंच पर आगमन से पूरी हुआ है। हर तरफ़ से पूँजी का आक्रमण है। हताशा की हालत तो है। हताशा एक सच्चाई है।
एक सामाजिक मैकेनिज़्म भी तैयार किया जाता है, जो इसके लिए दीर्घकालिक सहमति का माहौल बनाता है।
भारतीय जनतंत्र पूरी तरह धनतंत्र और अपराधतंत्र में बदल गया है। भ्रष्टाचार इस पूरी परिस्थिति का सूचक शब्द बन गया है, जब अण्णा हजारे जैसा कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन छेड़ता है, तो बहुत-से लोग यह जानते हुए भी कि इससे कुछ नहीं होगा, उसके अराजनीतिक आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो अराजनीति की राजनीति हो रही थी। आज पूँजी के अपने बृहत्तर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब राज्य और उसकी संस्थाएँ काफी नहीं हैं; उसे अनिवार्यतः अपराधियों की और अपराधतंत्र की मदद चाहिए।
यह काम जराइमपेशा छुटभैयों की सामर्थ्य और महत्त्वाकांक्षा से परे है। पूँजी को बड़े आपराधिक तंत्र को खड़ा करने, विकसित करने, हर तरफ फैला देने की दरकार है। पुलिस और सरकारी मशीनरी अपनी हद के भीतर ही काम कर सकती है। भले ही वह हदें तोड़ती रहती है, पर वहाँ भी हद है। आपराधिक तंत्र का काम उस हद के बाद शुरू होता है। सबसे पहले इसका लक्ष्य होता है नागरिकों के प्रतिरोध को तोड़ना और ऐसी दशा ले आना कि ज़्यादातर लोग नियति की तरह इसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लें। ये काम हमेशा डरा-धमकाकर या आतंक फैलाकर ही नहीं किये जाते, बल्कि एक सामाजिक मैकेनिज़्म भी तैयार किया जाता है, जो इसके लिए दीर्घकालिक सहमति का माहौल बनाता है।
भारतीय राज्य की आँखों के सामने, सरकार की जानकारी में दो समांतर तंत्रों–अपराध की मशीनरी और राज्य की मशीनरी — के बीच तालमेल बिना रिश्वत और भ्रष्टाचार के संभव ही नहीं। भ्रष्टाचार इस नये सिस्टम के लिए ऊर्जा का बुनियादी स्रोत है। इसके बगैर यह कारख़ाना ठप हो जायेगा। जब पानी सर के ऊपर से गुज़रने लगता है, और शहर का मध्यवर्ग भी बिलबिलाने लगता है, तो देवदूत की तरह अण्णा या रामदेव टाइप के उद्धारक प्रकट होते हैं। उनकी ख़ातिरदारी में तन-मन-धन से सबसे आगे कौन प्रकट होते हैं? कॉलोनाइज़र और बड़े बिल्डर लोग, कॉरपोरेट सी.ई.ओ., कॉरपोरेट एन.जी.ओ., व्यापारी मंडल और सबके पुराने सखा संघ परिवारी। तो विकल्प देने का काम भी उन्हीं का हुआ, जिनके कारण विकल्प की ज़रूरत पैदा हुई।
जनता में राजनीतिक चेतना जगाने का काम वामपंथी दलों का है और यह काम ज़रूरी होने के साथ-साथ संभव भी है, क्योंकि वामपंथी दलों की तमाम कमियों और कमज़ोरियों के बावजूद लोग अब भी परिवर्तन की उम्मीद उनसे ही करते हैं। हम जनतंत्र को लगातार सही-सही परिभाषित करते रहें और जनता को बताते रहें कि वास्तविक जनतंत्र क्या है, मौजूदा व्यवस्था जनतांत्रिक क्यों नहीं है, और उसे कैसे जनतांत्रिक बनाया जा सकता है। यह काम वामपंथी दलों और जनवादी संगठनों का है।मीडिया पर आधारित और मध्यवर्ग तक सीमित राजनीति के दायरे में बंद रहने के बजाय उन्हें ज़मीनी आंदोलन चलाने चाहिएँ। जो ज़मीनी आंदोलन जनता की वास्तविक समस्याओं के कारण पैदा हुए हैं और पहले से चल रहे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनमें हिस्सा लेना चाहिए।
भारत को विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कहा जाता है, लेकिन भारत की जनता का उससे केवल वोट देने तक का या हद से हद अपने अधिकारों के लिए आंदोलन और संघर्ष करने तक का ही संबंध है।
यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारे नेतृत्व में चलेंगे, तभी हम उनसे जुड़ेंगे। अगर वे आपको अपना नेतृत्व नहीं करने देते, तब भी आपका फ़र्ज बनता है कि उन समस्याओं पर अपनी राय सामने रखें, उनके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उन आंदोलनों से दूर-दूर नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े नज़र आयें। इसी तरह जनतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में लोगों का विश्वास बहाल किया जा सकता है।
आज लोगों में यह धारणा घर कर गयी लगती है कि सभी भ्रष्ट हैं, सभी स्वार्थी हैं, सभी चोर हैं। इसके चलते तमाम राजनीतिक दलों, संस्थाओं, नेताओं, कार्यकर्ताओं और सरकारें बनाकर शासन करने वालों पर से उनका विश्वास हट गया है। इससे जो शून्य पैदा हुआ है, उसे एक तरफ बाज़ार भर रहा है, दूसरी तरफ़ मीडिया और मनोरंजन उद्योग, तीसरी तरफ़ धर्म के नाम पर चलने वाला व्यापार, चौथी तरफ तरह-तरह के एन.जी.ओ. और पाँचवीं तरफ स्वयं को सिविल सोसाइटी कहने वाले लोग। लेकिन ये सब मिलकर जनता को और ज्यादा अराजनीतिक बना रहे हैं। ज़ाहिर है कि इससे देशी-विदेशी पूँजीपतियों को लाभ होता है, इससे स्थानीय तथा भूमंडलीय पूँजीवाद मज़बूत और टिकाऊ बनता है। इसी कारण इन तमाम गतविधियों पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर ये ज़मीनी आंदोलन हैं। जैसे ,बुनियादी अधिकारों के सवाल, विस्थापन से लड़ते , विकास की दिशा पर सवाल, जीने के हक़ और न्याय की माँग अधिकांश जन-आंदोलनों में वाम का ग़ैर-मौजूदगी न सिर्फ जन-आंदोलनों को अराजनीतिक दिशा में मोड़ती है। देश का शासक वर्ग — यानी सरमायेदार तबक़ा — अब जनतंत्र की परिभाषा बदलना चाहता है। वह जनतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रति लोगों में हताशा और विश्वासहीनता पैदा करने और उसे दोगुना-चैगुना करने में दिलचस्पी रखता है। वह दरअसल राजनीतिक तंत्र और समाज-व्यवस्था का फ़ासीवादी पुनर्गठन करना चाहता है।
मीडिया पर आधारित और मध्यवर्ग तक सीमित राजनीति के दायरे में बंद रहने के बजाय उन्हें ज़मीनी आंदोलन चलाने चाहिएँ।
अब तक, यानी बीस साल पहले तक, उसे यह संभव नहीं लगता था, पर अब यह पूरी तरह संभव लगता है। सरमायेदारों, दलालों और अपराधियों का क़ब्ज़ा हर जगह बढ़ गया है। यह सिलसिला वैसे तो इमरजेंसी के समय से ही शुरू हो गया था, पर चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह और अंतरराष्ट्रीय पूँजी के चहेते नरेंद्र मोदी के शासन काल में परिपक्व होते हुए और रफ़्तार पकड़ते हुए यह अब एक ‘क्रिटिकल मास’ अर्जित कर चुका है। नयी लफ़ंगी पूँजी भारतीय जनतंत्र का नृशंस पुनर्गठन कर रही है और पुराने और नये मीडिया घराने उसका साथ दे रहे हैं।
अख़बार, टेलीविज़न और सिनेमा के माध्यम से जनतांत्रिक तहज़ीब के विरुद्ध आक्रामक अभियान काफ़ी समय से जारी है। कुल मिलाकर यह संदेश दिया जा रहा है कि राजनीति भले लोगों की जगह नहीं है, कि यह ख़तरनाक धंधा है, कि आप कुछ नहीं कर सकते। यह प्रचार इसलिए सफल है कि यह लोगों के निजी अनुभव और व्यवस्था के भीतर उनकी तकलीफ़ों को छेड़ता है। लेकिन फिर वह उनकी भावनाओं को हमेशा एक प्रतिक्रियावादी, ग़ैर-जनतांत्रिक दिशा में मोड़ने की कोशिश करता रहता है।